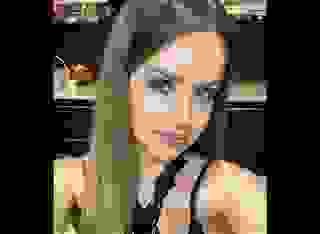Note: You can change font size, font face, and turn on dark mode by clicking the "A" icon tab in the Story Info Box.
You can temporarily switch back to a Classic Literotica® experience during our ongoing public Beta testing. Please consider leaving feedback on issues you experience or suggest improvements.
Click here’’ जी नहीं मानता। चाहता हूं तुम्हें अपने साथ भगाकर कहीं दूर ले जाऊं’’– मैने कहा।
वनमाला ने मेरी आंखों में झांका। एक चमक उभरी और एक मुस्कान तैर गई।
’’ क्यों ? मिल तो गया जो तुम चाहते थे। मुझे भगाकर अब क्या करोगे ’’– वह बोली।
’’ तुम मेरी प्यास हो। यूं चोरी–चोरी कब तक चलेगा ? तुमसे मिल पाना क्या सरल होगा ? सारा कुछ अनिश्चित है। क्या तुम्हें तसल्ली होगी ?’’
अभी–अभी तिरती चमक उदास हो चली थी। चेहरा उन बादलों से घिर चला था जो हमेशा उस पर छाए रहने के आदी थे।
’’ मैने वैसा कब कहा ? लेकिन आदमी की फितरत से मैं वाकिफ हूं। आखिर औरत हूं न! सपनों और हकीकत के बीच एक कठोर फासला होता है।’’
’’ अचानक यह बात कहां से आ गई ?’’–वनमाला की चिबुक थाम उसकी आंखों में झांकते मैने कहा।
दोहरी होती अपना मुंह उसने मेरी छाती में गड़ा दिया था।
’’ सब कहने की बातें हैं। भगाकर ले जाओगे कहां ? जिम्मेदारियों और मुसीबतों का अहसास होते ही तुम्हारी प्यास बोझ बन जाएगी और तुम भाग खड़े होओगे। हर मर्द यही करता है। जो है, वह है। उसे ही स्वीकार लेना चाहिये। क्या इतना काफी नहीं है ?– वह बोली।
अच्छे क्षणों के बीच आ चले वैसे कड़वे विचारों को मैने चित्त से झटक देना चाहा लेकिन उसमे कारगर न हुआ।
वनमाला का चेहरा मेरी छाती में धंसा था और उसे अपनी ओर खींचता मैंउससे चिपका पड़ रहा था। वह खुद भी आतुरता से लहराती लिपटती जा रही थी, लेकिन उसकी वाणी में बसा दार्शनिक गंभीरता में बुदबुदाए जा रहा था –
’’ जो इस वक्त हममें है, वह हकीकत है प्रियहरि। लेकिन मैं बताऊँ ? उससे भी बड़ी हकीकत यह है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। कर ही नहीं सकता। वह जिसे हम प्यार कहते हैं महज एक जुनून है। हर आदमी में एक वहशीजुनून होता है। अपने उस जुनून को ही वह प्यार का नाम देता है। इच्छा मेरी थी, इच्छा तुम्हारी थी। मैं और तुम तो एक–दूसरे के लिये अपनी ही चाहत के आलंबन थे। इच्छाओं की बेलें टकरातीं लिपट चलीं तो उसे हमने प्यार का नाम दे दिया। कल मेरी या तुम्हारी इच्छा का रुख बदल गया तो अपना प्यार इस बिस्तर से समेट हम कहीं और बिछा देंगे। समीकरण हटा कि प्यार घटा। तुम रूठना नहीं। लेकिन न जाने क्यो यह विचार मेरे चित्त में बार–बार आता मुझे बिखरा जाता है। मेरे प्यारे बुद्धूराम मैं जानती हूं कि मेरी बेरुखी, मेरे दूर–दूर भागते बच रहने से ही तो तुम मुझसे नाराज़ थे। मेरी भी इच्छा तुम्हारी इच्छा में समा जाने की उतनी ही बलवती थी, जितनी तुम्हारी। आखिर अंदर–अंदर छीलता अंतर का द्वंद्व जब असह्य हो गया तो मैने ठान लिया कि जो होना हो, वह होता रहे। मुझे समर्पण करना होगा और समर्पण पाना होगा। मुझे मालूम था कि तुम आओगे। आज वैसा हुआ। भविष्यको मैं नहीं देख सकती पर आज तुमसे मिलकर मैने राहत तो पा ली है।’’
मुझे अब तक नहीं मालूम कि रसरंग की वेला में वैसी बात की क्या प्रासंगिकता हो सकती थी ? क्या वनमाला मुझे विरक्त करना चाहती थी ? क्या वह खुद विरक्त होना चाहती थी ? क्या वैसा कहती वह प्यार में मुझे और अधिक डुबाना चाहती थी ? या क्या विश्वास और समर्पण में भीगती वह खुद मुझमें गहराई में डूब रही थी ,? जो भी रहा हो, वनमाला पर मुझे और ज्यादा प्यार उमड़ आया। उसका एक–एक शब्द मुझमें गहरे उतरता चला गया था। भविष्यमें क्या छिपा था मुझे भी नहीं मालूम था लेकिन उस वक्त मैने महसूस किया कि वनमाला उससे कहीं अधिक बुद्धिमती है, जितना मैं सोचता था। अपनी श्रेष्ठता का मेरा अहंकार खो गया था। मुझे निश्चयहो गया कि वनमाला का साथ ही सर्वथा मेरे अनुकूल है। उससे बेहतर सहचरी मिलना संभव न था। मैं उसे कभी न छोड़ूंगा और हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा।
शून्य में खोया समय अचानक हमारे बीच घुस पड़ा । वनमाला की नजरें घड़ी पर पड़ गई थी । ''बस, अब आज और नहीं, परे हटो ।'' उसने मुझे झटके से अलग कर दिया । मैं तृप्त था, मैं अतृप्त था । अचानक पैदा हुई रूकावट से सारा तनाव ठंडा तो पड़ गया, लेकिन वह एक अफसोसजनक उदासी भी भर गया था ।
विदाई के शब्द थे- ''आपको मैंने बहुत तरसाया था न । औरत की मजबूरी आप नहीं समझते इसीलिए रूठ जाते थे । आप क्या समझते हैं ? मेरे अंदर भी वही चाहत, वही आग, वही प्यास, तृप्ति की वही कामना थी । आपकी तड़प मुझे भी तड़पा कर रख देती थी ।''
वनमाला की आंखों से उमड़ते आंसुओं ने उसके स्वर को अवरुद्ध कर दिया था । रुंधे गले से उसने उस बेला के अंतिम शब्द कहे- ''आज मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है । आपको भारमुक्त करते आज मैंने भी मजबूरियों का सारा भार खत्म कर डाली है । आज हम दोनों तृप्त हुए । इस अवस्था में आकर अब तक बचती, वनमाला आपसे बंध चली है । स्त्री याद रखती है, पुरुष तृप्त होकर भूल जाता है । देखूं आप मुझे याद रखते हैं या नहीं ।''
यह कैसी मजबूरी थी कि वनमाला से मिलन की चिर-इच्छित बेला ने मिलने की प्यास बुझाकर प्यास की आग और भड़का दी थी । मैं सोच रहा था-'' क्या वनमाला के साथ मेरा मिलन यूं फिर कभी होगा ?''
दरवाजे से बाहर निकलती सड़क तक वह मुझे छोड़ने आई । श ाम का धुंधलका हो चला था । वृक्ष के नीचे अंधेरा गहराया हुआ था । मुझे बिदा करती वनमाला की चाहत से भरी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थी । वे भर आई थीं । आंसू के दो बूंदें गालों पर ढुलक पड़ी थीं ।
मैं तृप्त था मैं अतृप्त था. मेरी आँखें उसके चहरे में डूबी मुग्ध हैं . बाहर आँगन में उसके रंग-बिरंगे फूलों की छटा के साथ उसकी वाटिका की हरीतिमा वासंती धूप-छाहीं छटा में मनमोहक लग रही है. उस तरह सलाजता में ठिठकी वनमाला में भी मुझे वही छटा नज़र आ रही है. आँखों,पलकों,भौहों,होठों, गालों,लटों,नासिका – सब पर टिकती मेरी आँखें वनमाला को लील रही हैं. मुझे याद आ रहा है – “सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमा:”.
0000000000000000
कालोनी की आठवीं सड़क :
ठंड की गुनगुनी धूप का मौसम और दोपहर बाद का समय
उस दिन प्रियहरि लौट तो आया, लेकिन मन उसका वनमाला की कैद में ही रहा आया था । वह दिन-रात बेचैन रहता कि कैसे फिर वनमाला से उसका वैसा ही मिलन हो ? कैसे उससे मिलने की तरकीब वह करे ?, लेकिन सामाजिक मर्यादाएं, संकोच, उसके घर की पीड़ाएं, वनमाला के घर वाले का खयाल, उसके दूर के उस नए कालेज में जाने लौटने और मिलने का माकूल समय-ये सब के सब प्रियहरि का मन बांध देते थे । बहुत सोचकर उसने एक तरकीब निकाल ही ली । प्रियहरि को मालूम हुआ कि वनमाला की कालोनी की आठवीं सड़क में उसके एक परिचित गजानन रहते थे । उसने सोचा कि सहपरिवार गजानन के यहां जाने के बहाने वनमाला के यहां भी पहुंचा जा सकता है। इसे आप बेशर्म, दीवानगी की हद कह सकते हैं कि प्रियहरि ने वैसा किया भी। एक-सवा महीने के अंदर ही छुट्टी के किसी रोज अपने इरादे को पारिवारिक जामा पहनाते उसने सपत्नीक वनमाला के दरवाजे पर दस्तक दी ।
वह दिसम्बर का महीना था । ठंड की गुनगुनी धूप का मौसम और दोपहर बाद का समय । वनमाला प्रकट हुई । खोले गए किवाड़ के पल्लों पर टिकी उसकी कलाइयां और उनींदी आंखें लिए थके चेहरे की यादें प्रियहरि की आंखों में अब भी अटकी हैं । उसकी ही तरह सादगी में लापरवाही से पुराना स्लीपिंग गाउन उसके उन जिस्मों को ढके था जिनके पार झांकती प्रियहरि की पारदर्शी आंखें अपने तन को उससे चिपकाए रखना चाहती थी । उन ढलती गोलाईयों को उसने देखा जिन्हें मांज-मांज कर वह सख्ती और ताजगी से भर देना चाहता था । उसकी यही साधारणता मोहक थी। वह उस पुल का काम करती थी, जिससे दोनों के मन एक-दूसरे के साथ जुड़े थे । उस रोज घर बाधा रहित था । वनमाला और प्रियहरि की आंखें और दिल उनके बीच यादों भरे अतीत को देखते मौन संवाद कर रहे थे । लेकिन तब बीच में प्रियहरि की पत्नी थी, जिसकी मौजूदगी में व्यक्तिगत संभव नहीं था ।
कुछ ही देर में उनके बीच एक और मेहमान आ टपका था। वह उसकी पारिवारिक मित्र थी । पढ़ी-लिखी, जर्मन भाषा की अनुवादक एक ब्राम्हणी सम-वयस्का जो वनमाला के पति के बंगाली मित्र के साथ प्यार में ब्याह रचा वनमाला की मनःस्थिति लिए दिन काटती दिखाई पड़ रही थी । शादीशुदा जिंदगी की ढर्रे भरी नीरसता को उसकी बातों के अंदाज से प्रियहरि ने पढ़ लिया। नवागंतुका रमणी ने जिज्ञासा भरी दिलचस्पी से उन सब को देखा था और फिर बातों के सिलसिले चल पड़े थे । वनमाला को देखने की इच्छा उस दिन पूरी तो जरूर हुई लेकिन इस पूरी इच्छा ने दिलों की उस आस को अधूरा छोड़ दिया, उस प्यास को और अधिक बढ़ा दिया जिसकी तृप्ति के लिए प्रियहरि का मन छटपटा रहा था ।
भले ही वनमाला प्रियहरि की आंखों से ओझल हो चली थी। प्रियहरि के मन पर कब्जा उसी का रहा आया। घर-बाहर, सोते-जागते उसे वनमाला का प्यार, उसकी विवशता, उसका पशोपेश सालते रहे। हर पल बेकरारी में बीतता। कभी यह इच्छा होती कि भाग कर वह वनमाला के नए कालेज जा पहुंचे और कभी मन करता कि वनमाला के घर चला जाए। जी करता कि वनमाला से जा लिपटे और कहे कि प्रिये और परीक्षा ने लो। इस जन्म में अगर मिलना इस कदर मुश्किल है तो मेरे प्राण ले लो। तुम्हारी गोद में सर रखकर, तुम्हारे सांवले मुखड़े को निहारते लाचार उदासी में डूबी आंखों में आंखे डाले अपने प्यार में अंतिम स्वास लेना भी मेरे लिए परममुक्ति का क्षण होगा।
वे दिन ही ऐसे थे। चाहे वह बनारस विश्वविद्यालय में महीने भर रिसर्च के काम से रहा आया हो चाहे अपने संस्थान में सर खपाता बैठा होए या कहीं और व्यस्तताओं में रहा हो हर वक्त प्रियहरि को वनमाला की याद सताती रही थी। उन दिनों न जाने क्या-क्या और कितना वनमाला की स्मृतियों में उसने लिख डाला था।
साल भर बाद जब वनमाला फिर लौटकर आई तब प्रियहरि ने जुदाई के उन दिनों के एक-एक पल की गाथा उससे कह डाली थी। प्रियहरि के प्रेम में अभिभूत वनमाला ने वह सब सुना था। उसे अखबार के बहाने भेजे प्रियहरि के संदेश याद थे।
'हाय रे' की अदा में वनमाला प्रियहरि की इस दीवानगी से सराबोर कहती - ''आप भी तो बस ..........।'' बिछड़ने का दर्द और पुर्नमिलन की दीवानगी ने एक बार फिर वनमाला और प्रियहरि के ताल्लुकातों में बहार लौटा दी थी।
0000000000000000
औरत भला क्यों चाहेगी
कि उसका चहेता उसके किसी और रकीब के दर का ठिकाना उससे पूछे ?
वे दिन नवरात्रि और दशहरे की छुटि्टयों के थे । दिनचर्या से हटे इन दिनों में उस रोमांस का अभाव खटक रहा था, जो प्रियहरि को वनमाला के साहचर्य से मिलता था । वनमाला की याद बेतरह सताए जाती, लेकिन प्रियहरि पर अ-मिलन के ये पाँच-छः रोज ही भारी पड़ रहे थे । तीन-चार दिन बीतते न बीतते घर के उबाऊ अकेलेपन को भगाने प्रियहरि ने तरकीब निकाली । सामाजिक मेल-मुलाकात के बहाने अपनी बीबी को स्कूटर में बिठा वह पास ही के उस नगर को जाने वाली सड़क पर निकल गया जहां दूर-दूर बसे अंतरालों में उन ललनाओं का बसेरा था, जो उसका अतीत थीं । हालांकि सब से मिलने की आड़ में उसकी खास कसक उस वनमाला से मिलने की थी, जिसके यहां जाना संदेह को जन्म देता था । पहला डेरा सुंदरी जीनत के यहां पड़ा था, जो जहां भी होती अपनी सुंदरता और सलीके को अपनी जगह पर भी रच देती थी । उसकी सुंदर अभिरुचियों, कमनीयता और कोमलता की छाप उस घर में भी थी, जिसे विवाह के बाद उसने बसाया था। उस अंतिम छोर से लौटते एक पुराने सज्जन अधिकारी से मिलता वह विराग के यहां पहुंचा था । नीलांजना के घर का उसे ठीक-ठीक अनुमान न था । सीधी-सादी, विनयशीला नीलांजना को हालांकि प्रियहरि की बीबी ने एक-दो बार देखा था, वह उसे पसंद करती थी । जीनत और वनमाला से संबंधों और प्रियहरि के लगाव से वह परिचित थी । संबंधों के दौर में जब भी अपनी बीबी के संस्कारहीन विचित्र स्वभाव से बेरुख प्रियहरि अन्य मनस्क और उदास होता, जब भी प्रियाओं से बातचीत या लगाव के लक्षण या प्रमाण उसकी बीबी टोहती, अचानक उसमें एक गुनगुनाती गायिका प्रकट हो जाती । 'दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम चिड़ियों को डाले दाना' या फिर 'भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना' की गले में भी फंसी बेसुरी टेर से प्रियहरि वैसे मौकों पर बीबी की ईर्ष्या, उसके संदेह और तानों को खूब पढ़ सकता था ।
विराग के यहां से लौटते शाम ढल रही थी । चित्त में नीलांजना भी थी और वनमाला भी । वनमाला की राह पर संकोच में पड़ता भी वह खिंच चला था । उसका घर भी प्रियहरि के अपने घर की तरह अस्त-व्यस्त और झंझटों की छाया से घिरा हुआ करता था । प्रियहरि की बीबी के मन का गुबार जैसे प्रियहरि के मन तक धंसता समूचे वातारवण को खिझा जाता था, वैसे ही वनमाला के घर भी अजीब तरह के पशोपेश और संकोच की छाया उसकी अस्त-व्यस्तता में पसरी होती थी । बंगालियों के पूजा-पर्व का वह एक दिन भी वैसा ही था । नीम-अंधेरे में पति-पत्नी के अनमेल से उपजा उबाऊ उल्लासहीनता का वातावरण वहां प्रियहरि और उसकी पत्नी का स्वागत कर रहा था । आधी खुशी और आधे गम की मुस्कानें वहां थीं । जैसे उनके पहुंचने ने वनमाला और उसके पति को रोक लिया हो, वे संकोच में साथ बैठे । रसगुल्ले और नमकीन 'ना-ना' करते भी वे बाजार से ले आए गए थे । बीबी की उपस्थिति में सब कुछ पढ़ती भी आंखें उस सब को जुबान नहीं दे पा रही थी, जो प्रियहरि के दिल में था । अपने मिस्टर की छाया में वनमाला की हालत भी वैसी ही थी । औपचारिक बातें ही हुईं, सिवाय उन संवादों के जो प्रियहरि की बीबी और वनमाला के पतिदेव की मौजूदगी के बावजूद और उसकी आड़ में वनमाला और प्रियहरि के बीच एक-दूसरे की तारीफ में चले । वनमाला ऐसे उन पलों में खुश हुई जिनमें न जाने प्रियहरि की बीबी और रकीब के मनों में क्या चल रहा होगा । उन पलों में जैसे वे दोनों बातों में शरीक होकर भी अनुपस्थित थे ।
चलते-चलते प्रियहरि की बीबी बोली- ''नीलांजना के घर भी हो आते ना । यहीं-कहीं तो होगा ।'' प्रियहरि ने वनमाला की ओर देखा । उससे कहा- ''चलिए न आप भी साथ । हम लोगों ने तो घर देखा नहीं है ।''
वनमाला के कानों के लिए नीलांजना का नाम ज़हर था ।
वनमाला का मूड गड़बड़ा गया था । उसने तुरंत ने टाला- ''उसका घर तो बहुत दूर है । हम लोगों को भी ढूंढ़ना पड़ेगा । मैं तो वहां कभी गई नहीं । आप लोग चाहें तो हो आइए ।''
औरत भला क्यों चाहेगी कि उसका चहेता उसके किसी और रकीब के दर का ठिकाना उससे पूछे ? प्रियहरि बुद्धू था । सहज मन से वह वनमाला से तब पूछ तो गया था, लेकिन बाद में इस भूल का अहसास उसे हुआ कि वनमाला खुद उसे कितना और किस तरह चाहती थी यह वनमाला ही जाने, लेकिन यह तय था कि अपने चाहने वाले को किसी गैर की झोली में डालने वह तैयार न थी। प्रियहरि ने गौर किया तो पाया कि उसके मुआमले में सच भी वही था । उसकी प्रेमिका उसके घर आए और उसके रकीब का ठिकाना पूछती मिलने चली जाए - क्या प्रियहरि को वह भाता ? उस रोज नीलांजना रूट से बाहर हो गई थी, लेकिन इस चर्चा का जिक्र बाद में नीलांजना से प्रियहरि कर बैठा था । उधर वनमाला थी कि उस प्रसंग के बाद नीलांजना और प्रियहरि को साथ पा अपने आपको नाराज और प्रियहरि से कटी दिखने उतारू हो गई थी ।
888888888888888888
घर बनाम मकान
आदमी सारी दुनिया को जीत सकता है अपने घर को नहीं
Marriage is a romance in which the Hero dies in the first chapter. - Laurence J Peter
वनमाला घर में त्रस्त थी और प्रियहरि घर से बेजार। वनमाला को प्रियहरि हमेशा उसके अंदर छिपी प्रतीभा और गुणों की तारीफ करता प्रोत्साहित करता था। लिखने, रचने, पी.एच.डी. करने, संगीत सीखने कहता था। एक से एक योजनाएं प्रियहरि बनाता था लेकिन आंकाक्षा में उन सबको स्वप्नों की तरह समेटे वह कहा करती थी कि आप तो यह सब कहते है, लेकिन मेरे मिस्टर नहीं चाहते कि मैं कुछ करूं वे तो थोड़ी सी देर हो जाने पर जवाब-तलब करते है कि देर क्यों हुई ? वह प्रियहरि से कहती कि आप मेरे लिए व्यर्थ सोचते हैं। मैं पी.-एच.डी. नहीं कर सकती। मेरे मिस्टर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे लेकर हमेशा वे श क करते है। उनका बस चले तो कह दें कि घर से बाहर ही न निकलो। वह कह रही थी - ''मुझे कितनी तकलीफें है यह मैं जानती हूं। आप क्या समझते है ? आप जब मेरी तारीफ करते है तो क्या उन्हें अच्छा लगता होगा ? आपका खयाल गलत है आप के मुंह से मेरी तारीफ उन्हें बुरी लगती है। बंद कर दीजिए सोचना मेरे बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती।
इधर प्रियहरि का हाल भी कुछ वैसा ही था। अपनी अर्धांगिनी से उसके लिए कोई प्रेरणा नहीं थी। दोनों के व्यक्तित्व, रुचियां और संस्कार जमीन और आसमान की तरह की दूरी के थे। प्रियहरि अक्सर सोचता उलझकर रह जाता कि वह महज संयोग था या नियति का कर्ज जिसे चुकाने वह इस स्त्री से जुड़ा था। इस तरह वनमाला और प्रियहरि का मिलन त्रास और बेजारी के दो दिलों का मिलन था। प्रियहरि वनमाला में अपनी राहत ढूढंता था और वनमाला प्रियहरि में अपनी आकांक्षों के स्वप्न देखती तरसती थी। प्रियहरि अक्सर सोचा करता कि स्वप्न उसने भी घर बनाने के ही कभी देखे थे, लेकिन वे महज चिन्ताओं की उदास चहारदीवारी में कैद होकर रह गए थे।
किस्मत का लेखा भी अजीब होता है। चाहते आप कुछ और हैं और होता कुछ और है। न जाने कितनी जगह भटक कर प्रियहरि ने कितनी लड़कियां देखी थीं लेकिन जाकर टकराया वह सोमा से, जो उसकी पत्नी बनी। जल्द ही प्रियहरि को यह आभास हो गया था कि सुंदर शरीर में वह एक प्राणहीन मन थी। निबाहने के तब भी बहुत प्रयास उसने किये लेकिन वह असफल रहा। घर और परिवार के उसके सारे सपने चकनाचूर हो चले थे। जि़न्दगी उसके लिए यह अहसास बनकर रही आई कि वह अजनबियों के बीच एक ऐसे मकान का कैदी है, जिसने उसे केवल अपना कर्ज उतारने को बंधक बना कर रखा गया है। आदमी सारी दुनिया को जीत सकता है लेकिन अपने घर को कभी नहीं।
विवाह के बाद थेाड़े दिनों में ही यह उजागर हो गया था कि सोमा के पास महज कहने को स्नातकोत्तर की एक डिग्री तो है, मगर तीसरे दर्जे की वह डिग्री भी बराए नाम ही है। अपने विषय का न तो रत्ती भर ज्ञान उसे था ,और न उसमें उसकी कोई दिलचस्पी थी। आड़े–टेढ़े अक्षरों के साथ अपने दस्तखत भी वह प्रयत्नपूर्वक ही बना पाती थी। प्रियहरि का खयाल था कि सामान्य पृष्ठभूमि की घरेलू लड़की होने के लिहाज से वह घर को सजाने–संवारने में दिलचस्पी दिखाएगी, लेकिन वह भ्रम भी टूट चला था। निहायत बोझ की तरह घर की दिनचर्या के सामान्य काम सोमा निबटाती थी, और वैसा करते भी चेहरे पर वहखीझसे भरी होती।
प्रियहरि भी बेहद संघर्षों के बीच पला था। घर में झाड़ू लगाने, चूल्हा जलाने, रोज लालटेन की कांच को राख से मांजकर चमकाने, कपड़े धोने और खाना बनाने, मिट्टी खेादने और कुल्हाड़ी चलाते लकड़ी चीरने तक के संस्कार उसे बचपन से ही मिले थे। उसके लिये ये संस्कार अध्ययन औरशिक्षाके संस्कारों के अंग जैसे ही थे। उसे संघर्षों से भरा वह बचपन याद आता जब आठ–नौ साल की उमर से ही घर से बाहर रहते आश्रम की व्यवस्था में अपने हम-उम्र बच्चों के साथ पढ़ाई करते उसे नियत सारणी के दिनों मं। अपनी टीम के साथ दस–बारह साथियों की रसोई संभालनी होती। उसे आश्रम की हरे–भरे वृक्षों, पादपों और लताओं से सजी वह विषाल वाटिका याद आती जिसे संवारने में अपने सहपाठियों के साथ वह घंटों मिहनत किया करता था। उसे इन सब में भी उतना ही आनंद मिलता जितना उस नन्ही उमर में अखबारों, पत्र–पत्रिकाओं और साहित्य के अनुपम ग्रन्थों को पढ़ने और कपड़े की गेंद को हाकी या फुटबाल की गेंद बनाकर अपने साथियों के साथ मैच खेलने में मिलता था। तब अपना सामान लादे मन की मौज में सात–आठ मील का रास्ता तय करके आसपास के मौसमी मेलों या वनांचलों में पिकनिक मनाना उसके लिये मानों आमोद का भव्य आयोजन हुआ करता था। सामाजिक आयोजनों, सांस्कृतिक परंपराओं और देश–दुनिया की जटिलताओं को गहराई तक जाकर समझने में प्रियहरि की रुचि थी। सगे–संबंधियों, बुजुर्गों और विद्वानों का आदर करना उसके पारिवारिक संस्कारों में था। सामाजिक–पारिवारिक आयोजनों में उसके घर के सदस्य सश्रम सहभागी होते और इसके लिये उन्हेंप्रशंसाऔर सम्मान के साथ याद किया जाता था।
अपने सांस्कारिक अनुभवों पर प्रियहरि को गर्व था। वह उसका स्वाभिमान था। सुविधा–संपन्नता की संस्कृति से उसे बिचक नहीं थी, लेकिन श्रम और संघर्ष की संस्कृति के प्रति कथित भद्र–वर्ग की उपेक्षा और अलगाव की मनोवृत्ति उसे नापसंद थी। शायद यही कारण था कि वैसी संस्कृति के अभ्यस्त और पोषक सहचर और सहचरियों के निकट आने पर भी उनसे एक मानसिक दूरी उसमें प्राय: बनी रही। अपने इन्हीं संस्कारों में वह अपने घर को भी देखने के सपने देखता था।
सोचने और होने में बहुत फर्क होता है। बहुत जल्द उसने जान लिया कि सोमा घर के महज दैनन्दिन काम बसकिसी तरह निबटा जाने और शयन-सुख में मशीनकी तरह बिछाई जा सकने वाली मशीन जितनी ही अच्छी हो सकती थी। लगाव या अभिरूचि जैसी कोई चीज़ उसके स्वभाव में ही नहीं थी। यह मालूम हुआ कि तीसरे दर्जे की उसकी डिग्री थी और कागज–कलम से उसका नाता बस किसी तरह उस डिग्री को हासिल करने तक ही था। अपनी अनुरूपता में ढालने प्रियहरि ने उसे उत्साहित करना चाहा था कि वह आगे और पढ़ ले और विदुषी बने, लेकिन जबाब था कि वैसा करना अब उसके लिये संभव नहीं। उसे उसमें न रूचि है और न उसका कोई काम। जैसा साधारण लड़कियां अमूमन हुआ करती है शादी ही मकसद था। मकसद पूरा हो चला था और अब उसे करना ही क्या था? तीन के परिवार में पति और पत्नी के बीच प्रियहरि की मां बूढ़ी सदस्या थी। वह भोर हुए उठ जाती थी और दिन भर कुछ न कुछ करती अपने को व्यस्त और घर को व्यवस्थित रखा करती थी।
सोमा की जुबान उसके घुन्नेपन के कारण हिलने में आलस करती थी। दिन भर में प्रियहरि से ताल्लुकात में जुबान से रोबोट की तरह यंत्रचालित संक्षिप्त शब्दों का एक कंजूस समूह निकलता और संबंध की बस वही निशानीहुआ करती थी। प्रियहरि की अम्मा उस रोबो के लिए आरंभ से अवांछित तीसरा जीव रही आई। प्रियहरि के लिये यदि उसे शब्द होते –’’ खाना निकाल दूं क्या ? ’’, तो अम्मा के मुआमले में यह होता कि प्रियहरि के खा–चुकने के बाद एक संक्षिप्त सी थाली नि:शब्द लाकर सामने रख दी जाती थी। न तो दोबारा उससे जरूरत पूछने सोमा का सौजन्य होता और न तो मां की हिम्मत होती कि वह सोमा से कह सके। यह देखते प्रियहरि को बुरा लगता। वह चाहता था कि सोमा आत्मीयता से पेशआये, लेकिन जवाब में घूरती हुई उसकी उपेक्षा-भरी दृष्टि से वह टकराता। सोमा से कुछ कहना खीझ भरी बड़बड़ाहट को दावत देना होता था। गलती से कभी माँ को और ज़रूरत के लिए पूछ लेने की संकोच-भरी सलाह पत्नी को देने का दुस्साहस भी प्रियहरि को महँगा पड़ता था। चीखती हुई कड़वी जुबान फ़ौरन उलटकर हमला करती –
“ तुम चुपचाप अपनी थाली देखो। तुम्हारे कहे बिना वे भूखी मारी जा रही हैं क्या ?”
व्यवस्था पर सोमा का ऐसा आधिपत्य हो गया था कि सास की हैसियत बेचारी की हो चली थी। सोमा उससे यूं पेशआती जैसे दयावश ही प्रियहरि के यहां वह आश्रित रही आई हो। प्रियहरि को पहले वाकये से ही इसका आभास हो चला था कि सोमा पर लगाम लगाना कलह को दावत देना था।
वह दिन आज भी उसकी स्मृतियों में जीवित है। दोपहर बाद के करीब चार बजे का समय रहा होगा। मां ने प्रियहरि से इच्छा जताई कि एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा था। मां चाहती तो खुद भी चाय बना सकती थी लेकिन बहू का व्यवहार उसे रोकता था। अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी चीज में दूसरे का हाथ लगाना पत्नी को पसंद न था। प्रियहरि ने सोमा को जगाया कि चार बज चले है। अब वह उठ जाए और चाय बना ले। बजाय वैसा करने के सोमा ने नाराजगी से बड़बड़ाना शुरूकर दिया था –
’’ इन माँ-बेटे के कारण सोना भी मुश्किल हो गया है। अभी तो कुछ देर पहले खाना खाया है और इतनी जल्दी चाय की पड़ गई। ’’
प्रियहरि ने डांटा तो वह लड़ने पर उतारू हो गई।
’’ क्या समझ रख है तुम मां–बेटे ने कि मुझे दबा लोगे ? भूल में मत रहना। बताए देती हूं कि मुझे कम न समझना। मुझसे उलझोगे तो ठीक न होगा। ’’