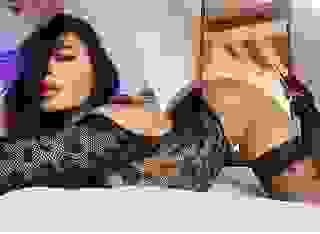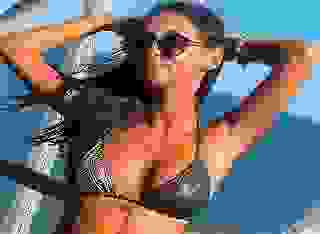Note: You can change font size, font face, and turn on dark mode by clicking the "A" icon tab in the Story Info Box.
You can temporarily switch back to a Classic Literotica® experience during our ongoing public Beta testing. Please consider leaving feedback on issues you experience or suggest improvements.
Click hereवनमाला ने सफाई दी -'' अरे वो तो मैने यूं ही कहा था । मैने किसी को इशारा नहीं किया । आप बेकार उसका बुरा मान बैठे। लगता है कि आप को गलतफहमी हुई है । फिर सिर झुकाए धीरे से वह आगे बोली -'' आप मेरी मुसीबत समझानेक की कोशिश क्यों नहीं करते ? मैं कैसे समझाऊँ ? आप को तो कोई कुछ कहता नहीं । लोगों को हमारा साथ-उठना बैठना बुरा लगता है ।''
उसकी बात ठीक थी । ज्यों ही कला और विज्ञान की कक्षाओं और आफिस के स्टाफ का आना शुरू हुआ वह चित्रकार संपादक-साथी आफिस में घुसता दिखाई पड़ा । उसने चुहल की - ''अच्छा तो आप लोगों की महफिल अब यहां जमने लगी है ,?''
जाहिर है कि खोजी निगाहें वनमाला और मेरे दिमाग में चुभने लगती थीं । जिस चोरी के लिए हमारे मन आतुर रहा करते, वह और निगाहों से पकड़ी जा रही थी । संकोच और खीझ से फिर हमने काम रोक दिया । आगे जो हुआ वह एक भयानक दुर्घटना ऐसी दुर्घटना, जो तूफान की तरह तब तक आगे बढ़ती रही जब तक उसने वनमाला और मुझे उन दो किनारों पर नहीं ला पटका, जहां से हम दोनों के पास आने की सारी संभवनाएं समाप्त हो चली थीं। उस तूफान के आवेग में कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। सारा कुछ उजाड़ हो चुकने के बाद अब मैं यह समझा सकता हूं कि तब वनमाला की ओर से जो कुछ होता चला गया था उनमें एक किंकर्तव्य-विमूढ़ता में निर्विकल्प असहाय स्त्री की मजबूरियां छिपी थीं। अपनी असहिष्णुता और अधीरता में तब मैं इतना अंधा हो चला था कि बार-बार समझाने के बावजूद अपनी समझ के दरवाजे मैने बंद कर लिये थे।
000000000000000
वह दिन मेरी नाराजगी का था
टूट गए दिखाई पड़ने पर भी जुड़ने-टूटने की दरम्यानी स्मृतियां कायम रहती है- एक अनन्त अफसोस से भरी पीड़ा के साथ ।
वह तकरीबन मई का महीना रहा होगा और ऐन वनमाला के पृथ्वी पर अवतरण की तारीख, जब अंतिम रूपरेखा तय करने मैने पत्रिका की समिति की बैठक बुलाई थी । सुबह परीक्षाएं नहीं थीं ? दोपहर में लोगों की ड्यूटियां लगी थीं । खयाल यह था कि केवल वनमाला और प्रियहरि प्रिंसिपल के कमरे में मौजूद होंगे और इश्क फरमाएंगे । नाम के लिए पॉंच-दस मिनट को औरों को बुला लेंगे । मैंने सूचना जारी कर दी थी । सुबह दस बजे वनमाला आ गई थी कुछ लोग और आ गए थे । मुझे उम्मीद थी कि वनमाला दिलचस्पी दिखाएगी और पहल करेगी, लेकिन नहीं । वह आई, स्टाफ रूम में एक दो मिनट रही फिर इधर-उधर चली गई । चित्रकारजी नहीं आए थे । इंतजार काफी हो गया था मैंने एक सहायक कर्मी नारायण से वनमाला को खबर भिजवाई कि वे आ जाएं । दिलचस्प जवाब आया कि और लोग यानी चित्रकार व्यास जी वगैरह आ जाएं तो साथ बैठेंगे ।
दो-अढ़ाई घंटे बाद मुझसे किसी ने आकर कहा कि सब लोग यानी व्यास, कामथ और (रूठी रानी) वनमाला प्राचार्य-कक्ष में आप को बुला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं । मेरा मूड उखड़ा हुआ था । प्रिसिंपल के सामने पहुंचा और अनजाने की तरह तलब किया कि क्या उन्होनें बुलाया है ? किनारे बैठे स्वनाम-धन्य मेरे सहयोगियो में से चतुर चित्रकार जी की मासूम आवाज आई- ''हां न सर, हम लोग सब यहां बैठे इंतजार कर रहे हैं । जल्दी से काम निबटा देना है, फिर परीक्षा की कक्षाओं में लौटना होगा ।''
वह दिन मेरी नाराजगी का था । खोजी निगाहों को तसल्ली देने वनमाला ने जैसे मुझे अपमान का मोहरा बनाया था । मैने स्पष्ट और दो टूक जवाब दिया कि मीटिंग दस बजे से थी और मुझे इंतजार करने अढ़ाई घंटे हो गये हैं । मैडम को ग्यारह बजे मैने खबर भेजी, लेकिन उनका मूड नहीं था। चीजें जब यूं चलती हैं कि सहायक ही परामर्श-दाता और काम करने वाले संपादक को चलाते चलें, बेरुखी दिखाएं तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। जहां किसी के मन में कटुता और दुर्भावना हो, वहां मैं काम नहीं करूंगा । आप जैसा बने खुद ही कर लें ।''
मेरा इशारा स्पष्टतः वनमाला की ओर था। जो बात की बात थी उसे वनमाला ने बखूबी, समझ लिया होगा । उसे उम्मीद न रही होगी कि संबंधों के आपसी मामले को लेकर वहां मैं उस तरह उससे पेश आऊँगा। वह केवल बड़ी-बड़ी पशोपेश भरी उदास आंखों से मुझे घूरती सुनती रही थी। उसके चेहरे पर शिकायत और पीड़ा की शिकन उतर आई थी। उसकी आंखें नम हो चली थीं। चित्रकारजी ने सफाई दी - ''नहीं सर, हममें से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा । आप नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे होगा ?''
उस दिन डॉ. नलिन से मैने वनमाला के व्यवहार पर दुख व्यक्त करते अपनी पीड़ा कह तो दी ही थी। वनमाला के व्यवहार से मुझे इस कदर वितृष्णा हुई कि मैने अभी हाल ही किसी पारिवारिक आयोजन पर स्टाफ की ओर से उपहार में भेंट किए सामूहिक चंदे से हिसाब लगाते हुए वनमाला का हिस्सा नलिनजी के हाथों में सौंप दिया। मैने कहा कि अब जब मैं किसी साथी के मन को अंदर तक झांक चुका हूं , तब उसकी झूठी सद्भावना और अहसान मैं नहीं कुबूल कर सकता। मेरा अब उनसे बात करने का भी ताल्लुक नहीं है इसलिये मिहरबानी करके यह उनका हिस्सा आप लौटा दीजिये।
वनमाला ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए मुझे यह समझाने की कोशिश की -''वह भेंट तो पारिवारिक है। उसे आप क्यों लौटा रहे हैं ? अगर कुछ है तो वह मेरे और आप के बीच है। गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। आपस की नाराजगी में आप चीजों को क्यों वहां तक ले जा रहे हैं ? वह अच्छा नहीं मालूम पड़ता। छोटी सी बात थी। मैं आप को कैसे समझाऊं ? आप ने न मुझसे बात की और न बात करने का मौका दिया। इतना बुरा आप क्यों मान गए ?''
बैठक से मैं बाहर निकल आया था । विग्रह और तनाव के उस दुखद परिदृश्य के बाद फिर डॉ. नलिन ने समझाने के लिए वनमाला को और मुझे बुलाया था । उनके सामने खुलकर बातें हुईं। मैने बताया कि ये आईं और बुलाने पर भी मेरे पास न आईं तो मुझे बुरा लगा था । वनमाला का जवाब था कि उसे किसी ने बताया नहीं । नारायण से बुलाने की बात की पुष्टि जब मैने उसी को बुलाकर की तो वनमाला ने दूसरा बहाना निकाला कि जब ये प्रियहरि खुद यहां थे तो क्या मुझसे बात नहीं कर सकते थे ? नारायण बाबू के हाथों खबर भिजवाने की भला क्या जरूरत थी ? क्या सचमुच नारायण के जरिए खबर भेजने से कोई गड़बड़ हुई ? क्या किसी ने उस पर से फिर वनमाला को छेड़ते हुए टिप्पणी की थी ? क्या उस संदेश की जानकारी किसी और की उपस्थिति में पाती हुई वनमाला पर किसी ने ताने कसे थे जिससे तिलमिलाती अपना गुस्सा वह मुझ पर उतार रही थी ? जो भी रहा हो, अपनी नाराजगी और विक्षोभ सरे आम वनमाला पर प्रदर्शित करता मैं कमरे से बाहर चला आया । वनमाला को आहत करते हुए बदले की तसल्ली के बावजूद मैं न जाने क्यों अपने आप में ही डरा हुआ और उदासी से भरा था ।
यह वही वनमाला थी जिसके लिए पिछले दिनों के उस खास पारिवारिक आयोजन के बाद वह मिठाइयां लेकर कालेज गया था । वनमाला के सम्मोह में खासतौर पर तैयार किये राजभोग का डिब्बा तब तक वहां उसने नहीं खोला था, जब तक वनमाला उसके रूबरू आकर खड़ी न हो गई थी । बड़े मनुहार के साथ पहला कौर उसने उसे वनमाला को यह बताते हुए खिलाया था कि मिठाई का वह डिब्बा तुम्हारी प्रतीक्षा में ही अब तक बंद रखा था । वह वही वनमाला थी जो मेरे आत्मीय बुलावे के बावजूद मेरे पारिवारिक आयोजन से बेरुख रही आई थी। वनमाला के लिये मेरा वैसा दीवानापन उसकी वैसी उपेक्षा के बावजूद रहा आया था।
मेरा चित्त अपार पीड़ा से व्यथित था । दुर्घटना का यह दिन उस प्रिया वनमाला का जन्मदिन था। उसे देखने, उससे मिलने और जाने कितनी-कितनी बातें उससे करने का मनोरथ लिये मैं कालेज में पहुंचा था। मैने कल्पना भी नहीं सोचा था कि यह दिन अचानक मनहूसियत की याद बनकर हमेशा के लिये कांटे की तरह मुझमें चुभन छोड़ जाएगा। वनमाला से विग्रह के बाद उस रोज़ सभी का चित्त उखड़ चला था। सभा भंग हो गई थी । सारा कुछ गुजर चला था लेकिन न जाने क्यों इस साहसपूर्ण झगड़े का मुझे मलाल था । वनमाला को चोट पहुंचाकर अफसोस से भरा मेरा मन रो रहा था । घटना के बाद जब होश आया तो न जाने किस प्रेरणा से मेरे कदम परीक्षा के कमरे में ड्यूटी पर तैनात वनमाला की ओर मुड़ गये थे । वनमाला को बाहर बुलाकर मैंने जन्मदिन की बधाई दी थी और उसे तकलीफ पहुंचाने माफी मांगी थी ।
वनमाला का मूड बिगड़ा हुआ था । ठीक अपने जन्मदिन पर अपना समझे जाने वाले प्रियहरि से कड़वे व्यवहार की उसे उम्मीद न रही होगी । अपने अपमान की चोट से आहत उसने प्रियहरि से बदला लिया -
''बस रहने दीजिए । सब के सामने आपका ड्रामा देख लिया । बच्चे नही हैं आप । आज सब के सामने आज मेरी इज्जत ले ली। ऐसा व्यवहार आप को शोभा नहीं देता। क्या करने आए हैं आप अब ? क्या और कुछ बाकी रह गया है ?''
मुझको ठंडा हुआ पाकर अब वनमाला की गर्मी शबाब पर आ चली थी। अपने अपमान का बदला अब उसी शैली में लेने वह उतारू हो आई थी जिसका प्रयोग दस मिनट पहले मैं कर गया था। वह धमका रही थी –
'' अब तो मेरा पीछा छोड़िए । समाज में आप की काफी इज्जत है। आप विद्वान हैं। बड़ा नाम है आप का। बचा रखिए उसे, अन्यथा एक दिन सब के सामने आप को मै भी नंगा कर दूंगी । जाइये आप, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है आप से ।''
दोनों के बीच इस दिन जो हुआ, उसपर कमरे में मौजूद उसके साथी परीक्षक उदयन का ध्यान गया होगा लेकिन बातें संभवतः सुनी नहीं गई थीं। अन्यथा प्रसारित जरूर होती। बहरहाल, खुली खटपट तो हो ही गई थी । उस दिन अपने को ''पत्रिका'' से मैने अलग कर लिया था। हां, -उससे ही, जिसे ''पत्रिका'' का अमूर्त नाम मैने आपसी प्यार से दिया था और जिसे मेरी वह पत्रिका बखूबी जानती थी।
संबंध क्या होते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह मालूम है कि टूट गए दिखाई पड़ने पर भी जुड़ने-टूटने की दरम्यानी स्मृतियां कायम रहती है- एक अनन्त अफसोस से भरी पीड़ा के साथ । नलिनजी ने भी उसके बाद मुझसे कुछ न कहा । बाद में उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर पत्रिका के लिए उनका प्रवचन और अपना संपादकीय चित्रकार साथी संपादक को सौंप दिया था । वनमाला पर से मेरा विश्वास टूट चुका था । मैने तय किया कि अब उस वनमाला के सामने भी नहीं पड़ूंगा, जिसे मेरा साथ तो क्या, शायद मेरे चेहरे से भी नफरत है । मैने भोलाबाबू से कहकर अगले साल के लिए अपनी कक्षाएं अब सुबह की जगह दोपहर के आसपास रखवाईं ताकि वनमाला के चले जाने के वक्त मेरा पहुंचना हो ।
भोलाबाबू बंगाल के कायस्थ थे । हर हाल में विनम्र रहना, झगड़े के बीच भी ठंडा दिमाग रखना और कुर्सी के प्रति श्वान की तरह वफादारी के गुण उसमें हैं । जहां और लोग केवल अपने सरकारी काम से मतलब रखते हैं वहां वह प्राचार्य के साथ चिपका रहकर दुनिया भर के काम बटोरते हैं और अपनी योग्यता और समझ के मुताबिक उन्हें निभा देते है । यह बात और है कि चापलूसी की उनकी वृत्ति और अतार्किक कार्य-पद्धति से स्टाफ के लोग, चाहे पुरुष हों या स्त्रियॉं, चिढ़ते थे । वनमाला के साथ संबंधों के अनुभव इस कदर कटु हो चले थे कि मुझे उनसे ही एक दिन कहना पड़ा था कि अगले साल का टाइम-टेबल इस प्रकार बनाए कि मुझे सुबह आना ही न पड़े, जिससे मैं नफरत और अजनबीपन के वातावरण से दूर रह सकूं । वनमाला कालेज छोड़ रही होगी तब मैं पहुंचूगा।
उस दिन भोला ने हंसकर मुझसे कहा था- ''तुम भी तो साले वैसे ही हो । मैने तो तुमको कई बार इशारा किया था, लेकिन तुम हो कि उसी से चिपके रहते हो । ये औरतें होती ही ऐसी हैं । पांव की जूती की तरह दबाए रखो तो ठीक रहती हैं । जितना ज्यादा मस्का लगाओगे और सर चढ़ेगीं । आखिर देख लिया न तुमने ? मै तो कहता हूं ऐसे लोगों से बात ही न करो । मैं तो जानता हूं इन लोगों को अच्छी तरह ।''
वह ठीक कह रहा था । इसीलिए शायद स्वार्थ के मौके पर छूट लेने महिलाएं प्रायः प्राचार्य से कुछ कहने की बजाय रियायत पाने भोला की खुशामद करना बेहतर समझती थी ।
मैने वनमाला से अपने को दरकिनार रखने का उस तरह इंतजाम तो कर लिया लेकिन तब भी क्या हुआ ? वह दूर सही, उसे देख लेने की मन में अभिलाषा तो बनी ही रही आई । रेल की जगह बस से ग्यारह बजे के करीब मैं पहुंचता इस मनःस्थिति के साथ कि-
हांफता हुआ भागता है मन
कि पहुंचूं
इससे पहले कि तुम निकल जाओ ।
महाविद्यालय मेरे लिए महज एक चेहरा है ।
जिसका नाम वनमाला है
प्रायः वनमाला के निकलते और मेरे पहुंचते मेरी आंख की पीड़ित करुणा और उसकी आंखों की शिकायत मौन की भाषा में मिलती रही और यूं दिन बीतते रहे । उस साल कालेज की पत्रिका से मैं गर्मियों के झगड़े के बाद अलग हो गया था । वनमाला से मेरे संबंध अब प्रायः नहीं रह गए थे । वह अनमनी अपने आपमें रही आती और अनमना मैं भी उससे दूर रहने की कोशिश करता । उससे तो कभी किसी की पटी नहीं, लेकिन मैं अपना गम छिपाये स्टाफ के दीगर मित्रों खासकर खूबसूरत स्त्रियों नीलांजना, मंजरी नेहा, वल्लरी, मंजूषा, सुरंजना अनुराधा से मिलता-घुलता रहा । यह बात और है कि उस मिलने और घुलने में भी अंदर-अंदर वनमाला ही दिलो-दिमाग में छाई होती ।
मेरे अंदर छिपी इस पीड़ा को सब जानती थीं । इसलिए पास आकर भी संभवतः इनके मन में वनमाला बीच में बनी रहती थी । न वे मेरे अंदर प्रवेश कर पा रही थी और न मेरा मन ठीक-ठीक उनमें रमता था । वनमाला एक थी, लेकिन सारी की सारी अन्य मेरे लिए एक सी थीं- मौका मिलने पर घायल हृदय की मरहम और मन के बदलाव की तरकीबें मात्र । वनमाला बोलती कुछ न थी, लेकिन उसे इस सब का आभास तो था । यदा-कदा वह औरों साथ मुझे घुलता, बातें करता देख प्रश्नवाचक दृष्टि से घूरती भर थी । एक मौन शिकायत कि मुझे तुम्हारी यह बात पसंद नहीं है । बातें तो उससे भी होती थी लेकिन न के बराबर और यदा-कदा ही, जिसमें न मैं ज्यादा खुल पाता था और न उसका दिल ।
000000000000
ईर्ष्या भी कितनी चमत्कारिक होती है?
''प्रियहरि, ये बताइये आप इतना अच्छा लिख कैसे लेते हैं ? मन को छू लेने वाले इतने मार्मिक शब्द आप लाते कहां से हैं । वनमाला की ओर एक निगाह डालती अनुराधा बोली- ''कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे तो पत्रिका में सब से अच्छा हिस्सा जो पढ़ने लायक है संपादकीय का ही लगा।''
महिलाएं इस बात पर आश्चर्य करतीं कि सनकी दिमाग वाली, अपनी अकड़ में औरों को तवज्जुह न देने वाली वनमाला से मेरी पटती कैसी है ? उनमें कहीं यह ईर्ष्या भी थी कि वनमाला से दिखने-सुनने, स्वभाव और आत्मीय व्यवहार में इनसे करीब रहकर भी वनमाला की ही मैं तारीफ क्यों करता हूं ? उसका सहारा ही क्यों लेता हूं ? वे यह बात मुझसे कहा भी करती थी लेकिन दिखाई पड़ते तकरार और मनमुटाव के बीच भी वनमाला और मेरी उपस्थिति के मौन क्षण और संक्षिप्त मुलाकातों के बीच साधारण सी दो चार शब्दों में हुई बातों का अंदाज ऐसा रहस्यमयी आत्मीयता का माहौल भर देता था कि हम दोनों के हृदय में उठ रही तरंगें औरों को शंकित कर देती थी । लोगों को यह समझने में देर न लगती कि कुछ न होने के बावजूद कुछ है । वह क्या है, इसे न प्रियहरि ठीक-ठीक जान सका न मेरी शुभचिन्तक ये कामिनियॉं कभी जान सकीं । पत्रिका छपकर कब तक वैसे ही पड़ी रही, इसका ठीक-ठीक अनुमान मुझे नहीं है । बस इतना याद है कि औपचारिक विमोचन के चक्कर में वह नवंबर तक लटकी रही । औपचारिक विमोचन के दौरान उस खास दिन मैने वनमाला को विशेषतः लक्ष्य करके द्वि-अर्थी संकतो में केवल चंद शब्द अपने वक्तव्य में कहे थे। बस इतना कि पत्रिका के विषय में मैं क्या कहूं ? अपनी पत्रिका के लिए जो कुछ मुझे कहना है वह मैने संपादकीय में कह दिया है । बात सामान्य ढंग से कही गई थी, लेकिन उसमें निहित संकेत क्या है यह वनमाला ही जान सकती थी । वह जानती थी कि प्यार में उसे मैने ''पत्रिका' 'का पर्याय बना दिया था ।
बातों-बातों में मैने कभी उससे पहले ही कह दिया था- ''प्यारी वनमाला, मेरी पत्रिका तो केवल तुम हो, जिसे मैं दिन रात पढ़ता हूं ।'' वनमाला के हृदय ने मेरा संदेश अच्छी तरह पकड़ लिया था । उसके बाद चाय के दौरान प्रिंसिपल के कमरे में जब मौजूद स्टाफ को पत्रिका के अंक बॉंटे गए तो मैने देखा कि वनमाला विस्मित प्रफुल्लता से संपादकीय के रूप् में अपने नाम लिखा मेरा प्रेमपत्र पढ़ रही थी ।
वनमाला से अब तक एक प्रकार का अबोलापन बरकरार था । वह अपनी रहस्यमय उदास अन्य-मनस्कता में क्या सोचा करती थी इसे जानना सदैव असंभव रहा है । यह जरूर है कि मेरी उदासी के साथ उसकी उदासी का सामना जब भी होता, समूचा माहौल दोहरी उदासी से भरकर मुझे और बेचैन कर देता था । मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि वनमाला ही नहीं, वनमाला और मेरे बीच संबंधों पर नजर रखने वाले करीबी लोग भी उन शब्दों के अर्थ समझते थे जो मैने विमोचन के उस खास दिन कहे थे और जिनकी तफसील संपादकीय में थी । यह बात दो दिन बाद की है । स्टाफ रूम में केवल हम तीन थे, वनमाला, मैं और अनुराधा । मैं बाद में पहुंचा था अनुराधा और वनमाला पहले से आसपास बैठी थी । पहुंचकर मैं भी उन्हीं के पास खड़ा हो गया था । वनमाला न होती थी तो उसे देखने की बेताबी और प्रतीक्षा होती । सामने होती तो उसके रहस्यमय उदास मौन की यातना से मन भारी हो जाता । मैने देखा अनुराधा के हाथ में कालेज की पत्रिका थी । देखा कि अनुराधा का चेहरा उल्लास की स्मिति से भरा था । मेरी उपस्थ्ति से वह स्मिति चहक में बदल गई थी जो कतई बनावटी नहीं थी । मुक्त मन से मेरी तारीफ करती वह संपादकीय के शब्द दोहरा रही थी ।
जैसे छेड़ रही हो, अनुराधा ने मुग्ध भाव से मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने कहा- ''वाह क्या बात है ?'' मुझसे मुखातिब होकर उसने पूछा - ''प्रियहरि, ये बताइये आप इतना अच्छा लिख कैसे लेते हैं ? मन को छू लेने वाले इतने मार्मिक शब्द आप लाते कहां से हैं । वनमाला की ओर एक निगाह डालती अनुराधा बोली- ''कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे तो पत्रिका में सब से अच्छा हिस्सा जो पढ़ने लायक है संपादकीय का ही लगा।''
अनुराधा के शब्दों को सुनती बगल ही उदास अन्यमनस्क खड़ी और वैसे ही पुस्तक के पन्ने पलटती वनमाला के चेहरे पर जल्दी-जल्दी कुछ भाव आए और गए । उसकी सूनी आंखें मुझे देख रही थी और मेरी आंखें उस क्षण उसकी आंखों के सूनेपन में झांक रही थीं। मुझे ऐसा कुछ आभास हुआ जैसे मेरे पहुचने से पहले अनुराधा और वनमाला के बीच कुछ निजी संवाद हुए हो सकते हैं।
मैने अनुराधा को धन्यवाद दिया । कहा -'' यह तो आप समझती हैं । जिन्हें समझना है, वे भी समझें तब तो।''
बाबजूद इसके कि अनुराधा का बीच में होना वनमाला और मेरे बीच पुल का काम कर रहा था या अनुराधा ही खुद जानबूझकर उस क्षण हमारे बीच पुल बनी हुई थी, मैने इसी में भलाई समझी कि गर वनमाला को मैं पसंद नहीं हूं, अगर वह अपनी अकड़ में अबोली है तो उसके अनप्रेडिक्टबल मूड को नहीं छेड़ना ही ठीक है । अबोलेपन की दूरी मैने बरकरार रखी और तुरन्त पुस्तकें उठाकर कक्षा में चला गया । मन में एक चीज फिर भी भर गई कि जिस पर मैं मरता हूं,, जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसके लिए मेरे शब्द अर्पित हैं, वह कितना निष्ठुर है कि सारा कुछ जानकर भी उसके मुंह से बोल नहीं फूटते ।
कला की कक्षाओं का वह पहला घंटा था । अपनी कक्षा लेकर ज्यों ही मैं निकलने को हुआ वनमाला की कक्षा का एक छात्र मनोहर दरवाजे पर टकराया- ''आप को वनमाला मैडम ने बुलाने मुझे भेजा है ।''
मुझे अचरज हुआ और आश्चर्य से भरी खुशी भी कि आज कौन सा शुभ मुहर्त है, जो मेरा प्यारा दुश्मन मुझे संदेश भेजकर बुला रहा है । स्टाफ रूम में जाकर मैं अपनी जगह बैठ गया, लेकिन बात की पहल मैने फिर भी नहीं की । तभी बहुत दिनोंसे अबोली वनमाला अपनी जगह से उठ मेरे पास आ खड़ी हुई।
उसने कहा- ''एक चिट्ठी भेजनी है, आप मुझे लिखा दीजिए ।''
न जाने क्यों अच्छे क्षणों में भी वनमाला के अनिश्चित मूड की छाया बनी रहती है । क्या यह मेरा मान था कि दिल में अच्छा लगने पर भी मैने विनम्रता से उसे टाला-
''आप तो अच्छा लिख लेती हैं लिख लीजिए ना । कोई खास बात तो है नहीं इस विषय में''- मैंने कहा ।
वह जिद की मनुहार में बोली- ''नहीं आप ज्यादा अच्छा लिखते हैं । आप मुझे बोलिए मैं लिखूंगी।''
पत्र सामान्य संदर्भ में था । छात्र की किसी प्रतियोगिता के लिए छात्रों नाम भेजने थे । मैने लिखाया वनमाला ने लिखा । मैं वनमाला को निहारता रहा। कुछ भी तो नहीं बदला था। उसका वही गुमसुम उदास चेहरा । अनबोले भी बहुत कुछ कहतीं उन्हीं खोई आंखों की मुझमें समाई पड़ती वैसी ही भेदक दृष्टि। मैने सोचा कि ईर्ष्या भी कितनी चमत्कारिक होती है । अपना अबोलापन तोड़कर वनमाला का खुद ही मेरे पास चले आने की पहल मात्र मेरे लिखे संपादकीय के सांकेतिक प्रेमपत्र में निहित भावनाओं की अभिस्वीकृति थी । मैं चाहता था कि उसकी छाती पर सिर रखकर रोऊँ । लेकिन वैसा कर न सका । न जाने कितने द्वंदों से घिरी वनामाला उदास थी । संकेतों को जुबान वह न दे पाई । लिपि और ध्वनि रहित भाषा में उस दिन सारा कुछ छिपा कर भी वनमाला जैसे सारा कुछ कह गई थी और मैने सब सुन लिया था- ''तुम इतने उदास क्यों हो ? मुझे भी तुमसे उतना प्यार हैं, जितना तुम्हे मुझसे है । अनुराधा की बातों पर क्यों जाते हो ? तुम तो मेरे हो, केवल मेरे । मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता । तुम मुझसे क्यों रूठ जाते हो । भले ही मैं तुमसे नहीं बात करती, मेरा दिल तो करता है । नादान पिया, तुम इतना तो समझा करो । मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ ? काश मेरी मजबूरियां तुम समझ पाओ।''
हां, यह भी वनमाला ही थी । वही वनमाला, जिसकी रहस्यमय खामोशी और अचानक प्रकट होनेवाली क्रूरता से मेरे प्राण निकल जा रहे थे । मुझे ऐसा अब लगता है कि उस दिन अनुराधा की मेरी तारीफ आकस्मिक नहीं थी । अवश्य मेरे पहुंचने से पूर्व वनमाला से अनुराधा की बात गुपचुप हुई होगी और वनमाला के ढ़ंडेपन के खिलाफ मेरे सामने ही मेरे लिखे की तारीफ सप्रयोजन की गई होगी । प्रयोजन या तो वनमाला के मन में ईर्ष्या जगाना रहा होगा या वनमाला के ठंडेपन को कोसना । रूठने और मनाने का यह खेल वनमाला के साथ मानो शाश्वत हो चला था । उसके दिल में क्या था यह समझना मुश्किल था । ऐसा लगता है जैसे स्त्री और पुरुष के बीच यह खेल प्रकृति से ही रचा गया है । स्त्री बचती है, भागती है, ठंडी बनी रहना चाहती है और पुरुष उसे समेटना चाहता है, उसका पीछा करता है और उसके गर्म होने का इंतजार करता हाय-हाय करता है । समाज का भय, नैतिक मर्यादाएं परिवार की उलझने चहारदीवारी की कैद, गर्भ का भय, और इन सब से ऊपर जॉंघो के बीच छिपी इज्जत को खजाने की तरह संभाल रखने की सीख स्त्री पर हमेशा हावी रहती है । यही कुछ होगे जो वनमाला के मन में बचाव और समर्पण के बीच द्वन्द और खीझ में समाए रहते थे । पशुओं के जगत में भी इसे आप ठीक वनमाला-वृत्ति के रूप में देख सकते हैं । मादा कभी पहल नहीं करती । कुत्तों और सांड़ों के झुंड अपनी मादाओं के पीछे भागते हैं । वे बचती हैं, भागती हैं, गुर्राती हैं, काटती हैं और बमुश्किल उन पर पीछे भागता नर सवार हो पाता है । मनुष्य की जात में समाज, परिवार और नैतिकता की बाधाएं हैं, लेकिन पशुओं के समाज में तो नहीं । फिर वैसा क्यों होता है ? शायद नर और मादा की प्रकृति के बीच यह भेद शाश्वत ही है ।
जब वनमाला अकेली होती, पकड़ में आती और घर के तनाव से मुक्त होती तब वह अच्छे से पेश आती । प्यार की बातों पर वह चुहल करती मजा लेती, तरसा-तरसा मन में और प्यास भरती थी । लेकिन जब अवसादग्रस्त और परेशान होती तो जुबान पर कोई नियंत्रण न रहता । इसी खेल के बीच एक रोज सुबह-सुबह मैं फिर फोन कर बैठा । किसी समारोह में एक रोज उसी के नगर रहकर ही लौटा था । वहां रहते ऐसा मन करता कि उसके घर घुस जाऊं, लेकिन ''मन का करना'' बस लाचारी ही है । न रहा गया तो दिल की बातें कहने की बेताबी में फोन लगा बैठा । मेरा अनुमान गलत था । वह घर से कालेज के लिए निकली तो न थी, लेकिन उसके मिस्टर घर पर ही थे । जरूर उसे फोन पर जाता देख उसने व्यंग्य किया होगा ।