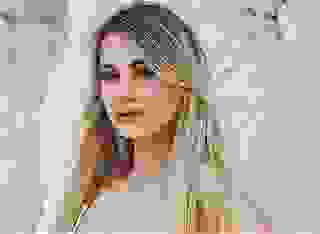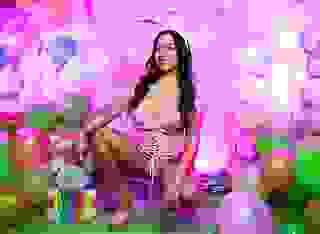Note: You can change font size, font face, and turn on dark mode by clicking the "A" icon tab in the Story Info Box.
You can temporarily switch back to a Classic Literotica® experience during our ongoing public Beta testing. Please consider leaving feedback on issues you experience or suggest improvements.
Click hereजहां तक याद पड़ता है जीनत भी अपने को 'वर्गो' कहा करती थी, जैसा कि प्रियहरि तो था ही। उन दोनो में कहीं कोई कमी न दिखाई पड़ने पर भी एक खालीपन रहा होगा जिसे वे परोक्षतः महसूस करते थे। जाती तौर पर जीनत के निजी और भावनात्मक संबंध विराग से थे। तब भी किसी खास मौके को छोड़ खुले रूप में वह प्रियहरि को कभी न दिखाई पड़ा था। जीनत का व्यक्तित्व खुला था और सभी से वह पूरी गरिमा, नफासत और खुलेपन से पेश आती थी। जिस एक बार का जिक्र है उसमे भी गवाह दो ही थे - एक खुद प्रियहरि और दूसरी जीनत। हुआ यूं कि एक दिन जीनत के निजी मातहत ने आकर प्रियहरि को खबर दी कि मैडम उसे बुला रही हैं। सुबह का वक्त था और माहौल शायद जनवरी - फरवरी के गुनगुने ठण्ड का, जब पढ़ने वालों की आमद-रफ्त कम हो जाती है। प्रियहरि उसके कमरे में गया तो उसे सामने बिठाकर जीनत ने विराग की बेरुखी की शिकायत करते हुए यह कहा कि प्रियहरि उसे समझाये। जीनत का कहना था कि उसकी शादी कहीं और तय करने पर उसके घर में लोग आमादा हैं। उस वक्त जीनत कमजोर हो चली थी। प्रियहरि को समझाते उसकी भावना का बांध टूट गया और आंखों से मोती झरने लगे। प्रियहरि के सामने टेबिल पर कलाइयां फैलाए उसने सिर झुका दिया और सिसकती रही। प्रियहरि ने बड़े प्यार से उसे समझाया, उठाया, तसल्ली दी और कहा कि मैं विराग से बात करूंगा। लोगों की आवाजाही में उस दिन तो बात न हो सकी, लेकिन बाद में प्रियहरि ने ससंकोच विराग को वह बात बताई और समझाया कि जीनत का ध्यान वह रखे। विराग ने अविचलित भाव से सुना और बस इतना कहा कि ''मैं देखूंगा।''
जीनत के पास आते-आते प्रियहरि ने दो-तीन कविताएं उस पर लिख डाली थीं। उन्हे बड़ी रूचि से जीनत ने सुना और उनकी तारीफ भी की। जीनत को प्रियहरि की एक मात्र और सबसे अच्छी भेंट उसकी वह एक कविता ही थी ,जिसमें प्रियहरि ने निहायत खूबसूरती से जीनत की तस्वीर खींची थी। वह इतनी खुश हुई कि कविताओं के ढेर से उस खास कविता को पसंद कर उसकी स्क्रिप्ट प्रियहरि से उसने आग्रहपूर्वक फ़ौरन ही छीन ली थी। जीनत की यह खूबी थी कि वह शातिर औरतों की तरह नज़ाकत और अदाओं का इस्तेमाल कर प्रियहरि को प्रभावित नही करती थी, गोकि ये चीजें उसमे थीं। शायद इसीलिए उसे वैसा करने की जरूरत ही नही थी। उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी में ही कुदरत ने इन्हें निखार कर रख दिया था। यह शेर कहा भले ही किसी ने चुहल के रंग में है, लेकिन जीनत पर यह बिना किसी बनावट के लागू होता था कि- ''खु़दा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है।''
उस समय जीनत के अलावा नीलान्जना और चन्द्रकिरण उर्फ रोज़बूटी भी थी। वह इतनी गोरी-चिटटी, सहज और आकर्षक थी कि वनमाला की ओर किसी को ध्यान देने की फुरसत ही न थी। न जाने कौन सी परिस्थितियां थीं जिनसे वनमाला यूं गुमसुम और गम्भीर दिखाई पड़ती थी कि वह अपनी उम्र से कहीं बड़ी प्रौढ़ा नारी ही लगती। इसकी छिपी नजर चंचल चित्रकार कानन पर दिखाई पड़ती थी। इधर कानन था कि औरों की तरह वह भी सर्वोत्तम यानी जीनत की तारीफ करता था। वनमाला का प्रसंग छिड़ने पर नाक-भौं सिकोड़ता वह हंस पड़ा था - ''वह! वह तो मुझे बुढ़िया लगती है।'' व्यक्तिगत प्रसंगों में चन्द्रकिरण को प्रियहरि प्यार से रोज़बूटी या स्वीट-डॉल कहकर पुकारता था। चार फुट दस इंच की पैंतीस किलो वजनी बड़ी-बड़ी भूरी आंखों वाली यह गुड़िया बला की खूबसूरत थी। किसी एक रोज सूने में दोनों ही आ भिड़े थे. कोने में कद नापने का फूटर रखा था. न जाने क्या सूझा वह उसके पायदान पर चढ चली. साथ चिपके तरंगे कुछ इस तरह बदनों में तैर रही थीं कि प्रियाहरि ने उसे अवस्थित किया और ठुड्डी थाम नपने को सर पर जतन से संवारे बालों पर ला टिकाया. चार फुट दस इंच .
“ मैं भी तो देखूं “ प्रियहरि ने कहा . सटकर खड़ी रोज़बूटी ने प्रियहरि के सर को वैसे ही ठुड्डी से उठा ताना और नाप लिया.
“पांच फुट सात इंच.” रोज़बूटी ने उच्चारा .
उसकी खूबसूरत आँखों और गुलाबी बारीक होठों पर खुशी, हया और चंचलता को एक साथ समेटे मुस्कान तैर उठी थी. नज़रें उठतीं अर्थपूर्ण संकेतों को समेटे प्रियहरि की नजरों से मिलीं जहाँ वैसी ही तरंगें लहर रही थीं जिन्हें रोज़बूटी संजोए थी. वह मुस्कुराई. उस गोपन मुस्कराहट में सन्देश साफ छपा था.
उसे उच्चरित प्रियहरि ने किया – ‘जोड़ी ठीक बनी. नाप एकदम फिट है.’”
उस रोज़ फिर सारा समय औरों की भीड़ आ चुकने के बाद भी बार-बार टकराते दोनों के बीच मिलते और टकराते नयनों का रहा. वह एक पल ऐसा रहा कि फिर हर मिलन में कद मिलान की चाहतें फिर-फिर कि दिलों के दरम्यान हिलोरें मारतीं. पल चमत्कारी होते हैं . कभी-कभी एक पल वह कर जाता है जो प्रयत्नों के बावजूद जीवन भर भी संभव नहीं पाता. रोज़बूटी के साथ संयोग में गुजरा वह एक पल फिर दोनों के दरम्यान ऐसा स्थायी हो चला कि जब तक वह साथ रही खुशियों की बहार के दिन रहे. परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई थीं कि विवाह की बेसब्री में डूबी रोज़बूटी का पड़ोसी और निजी हिस्सा बनता चला गया था. वह किस्सा बाद में कहना ठीक रहेगा। अभी मैं जीनत की ओर चलूँ.
दरअसल जीनत से प्रियहरि के संबंध दिनोंदिन ऐसे गहराते गये थे कि विराग को छोड़ वह प्रियहरि की रागिनी बन चली थी। कई बार ऐसे मौके आये जब दिल से बेकाबू जिस्मो-जां की ओर वे बढ़ चले, लेकिन मिलन की अधीरता को अचानक थाम जीनत कह बैठती - ''प्रियहरि, रहने दो ना प्लीज़। अपनी जीनत की बात मानलो। मैने सब कुछ किया है लेकिन वो काम मैने अभी तक नही किया है। मुझे बहुत डर लगता है। मैं अभी भी उस मामले में पाकीजा हूं ''
वो काम'' के मसले में जीनत का आशय वे दोनों समझते थे। उस काम को मन में छिपाए और कल्पनाओं में देखते प्रियहरि और जीनत के पास मन को मसोसने के अलावा कोई चारा न होता।
बदकिस्मती यह कि जीनत को जल्द ही प्रियहरि से बिछड़ना था। जीनत का तबादला कहीं और हो गया था। यही नहीं, उसकी शादी भी मर्ज़ी के खिलाफ कहीं और तय हो गई थी। जीनत मायूस और टूटी हुई थी। ज्यों-ज्यों उसकी शादी की चर्चाएं बढ़ीं, जीनत बेहद बेचैन और द्वंदग्रस्त होती चली गई थी। तनहाई में उदास बीते दिनों की यादों में वह रोया करती। इन्ही दिनों किसी एक दिन जीनत से प्रियहरि की अंतिम मुलाकात हुई थी जो उसकी स्मृतियों में इतिहास बनकर हमेशा के लिए थम गई है। विचित्र परिस्थितियों में हुई वह दिलरसाई की दिलचस्प मुलाकात थी। प्रियहरि के चित से जीनत के साथ अंतिम मिलन की उस प्यारी घटना का उतरना मुश्किल था। हां वह ,जब जीनत का पाकीज-वर्जित जीनत और प्रियहरि के बीच खेल-खेल में ही जन्नत के बाग का वह मीठा फल हो गया था, जिसके स्वाद की हर पुरुष और स्त्री में तरस होती है। उसे अब वह भूल जाना चाहता है।
जीनत की शादी का कार्ड प्रियहरि को मिला था। न जाने क्या कश्मकश थी कि प्रियहरि जीनत के उस रूप के सिवा, जो केवल उसका अपना था किसी और रूप में बर्दाश्त
न कर सकता था। वह नहीं गया। प्रियहरि के साथ ही सारे और चाहने वालों के दिलों में अपवित्र खलबली मचाती जीनत अपनी पवित्रता साथ लिए उन्हें छोड़ चली गई थी। यह अजीब किस्मत थी कि वह प्रियहरि को जैसे वनमाला के हवाले कर चली गई थी। उसका साथ छूटना ही वनमाला से प्रियहरि का मिलना था। बहुत बाद में वनमाला के प्रेम में डूबे प्रियहरि के दिल ने जब अपना सारा कुछ कविताओं में ढाल दिया तो अजीब था कि छपाई से पहले चयन और संपादन में प्रियहरि को जीनत ही याद आई। जीनत ने उन्हे खूब पसंद किया, चुनाव किया, अपनी राय दी, लेकिन यह अजीब था कि प्रियहरि की दूसरी प्रिया बंगाल का जादू वनमाला पर रची कविताओं के प्रति जीनत ने हौले से अपनी बेरुखाई साफ जाहिर कर दी थी। प्रियहरि जीनत से कैसे कहता कि कविताओं का जो अनुवाद उसके हृदय ने रचा, वह उसके नाम होता अगर समय के फेर से चिपकी वह उससे जुदा न हुई होती । जो भी हो जीनत किसी भी हृदय का प्यार हो सकती थी। वह इतनी अच्छी, प्यारी ओर खूबसूरत थी कि उसे भुलाना प्रियहरि के लिए कभी संभव न होगा।
जीनत का जाना प्रियहरि की सोहबत के लिए एक खलिश थी, जो बहुत दिनों तक बनी रही। तब-तक, जब-तक वनमाला उसके बहुत करीब न आ गई। वनमाला के करीब आने की आहट तो प्रियहरि के दिल को थी लेकिन प्रियहरि और वनमाला दोनों ने उस दिन लगभग उसे तस्लीम कर लिया, जिस दिन की यह घटना है।
00000000000000000000
समूचे बचपन में फैले हुये थे
झांपियों और अंधेरे खंडहरों के वे दिन
आरिफ के कहने पर ही प्रियहरि वहां आया था। कहां उज्जयिनी, कहां, भोपाल, और कहां कोलिकाता और फिर यह जगह ? उसे कल्पना भी नहीं थी कि यही उसकी जिन्दगी का लंबा और निर्णायक पड़ाव होने जा रहा है। तब भी क्या वह बदल सका था ? शायद नहीं। अतीत उसे अब भी सम्मोहक लगता था। स्मृतियों में जीता अब भी वह अपने को अलस्सुबह हाथ में फूल लिये गोपाल मंदिर की ओर भगाता हुआ पाता था। सुबह और शाम की आरती पर उच्चरित समवेत स्वरों के साथ आगे-पीछे हाथ लहराते हुए काठ के हथौडे से घंटे पर टंकार की लय देता वह यूं डूब जाता कि जैसे गोपालजी मोर मुकुट धारे अभी-अभी मंदिर में प्रकट होने वाले ही हैं।
तब वह घनघोर रूप में सदाचारी था हालांकि घर में अचार या सींगदाना खरीदने आई अपनी समवयस्का सलमा की झुकी आंखों में तैरती चमक से चमत्कृत प्रियहरि का दिल तब उसे गिनने की हिदायतों के होते भी सलमा के हाथों गिनती से कुछ अधिक सौंप जाता था। सलमा कुछ समझकर तिरछी नज रों से उसे निहार दबे होठों से मुस्कुराती और प्रियहरि से वैसी ही भाषा में जवाब पा खुश होती और खुश करती लौट जाती थी। प्रियहरि के परिवार जैसी ही सलमा के परिवार की स्थिति थी। न तो वे इतने संपन्न थे कि उन्हें पैसे वाला कहा जा सके, न इतने विपन्न कि गरीबों की तरह उन्हें गिना जा सके। प्रियहरि को इसका इसका आभास था कि सलमा मुसलमान है, लेकिन जब वह उसके सामने होती तो वह खुद को और सलमा को अपने-अपने दायरों से बाहर पाता था। वहां धरम दोनों तरफ आंखों की चमक और ओठों की मुस्कान में आलिंगित हुआ एक हो जाता था। वैसे भी उसे अपने मोहल्ले में हिन्दू और मुसलमान कभी मजहब के रंग में नज र नही आते थे। वेशभूषा और जुबान से गर पहचान उभरती भी तो वह छोकरे और छोकरियों, गरीब और अमीर की पहचान से कमतर हुआ करती थी।
प्रियहरि के पिता शुद्धतः महात्मा गांधी के अनुयायी और आजादी के पहले के कांग्रेसी संस्कृति के थे। साहित्य और संस्कृति के वे गहन अध्येता थे। आजादी के आंदोलन में तब के बड़े-बडे रहनुमाओं के साथ उन्होंने दिन गुजारे थे। उन्होने असहयोग और सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौर में सैकडों मील की पदयात्राएं की थीं। अपने खास मित्र जो किसी एक विशेष संप्रदाय के संत थे की प्रेरणा से एक विशालकाय ग्रंथाकार के संचालक भी वर्षों तक रहे आए थे। अंग्रेज अधिकारियों के छापे के दौरान किस चतुराई से उन्होंने सारे प्रतिबंधित ग्रंथ छिपा लिए थे इसका जिक्र वे बडे गौरव से किया करते थे। युद्ध और शांति, अन्ना कैरिनिना, नाटरडैम का कुबडा, अपराध और दंड , बूढा गोरियो, पिता और पुत्र, गाडी वालों का कटरा, टाम काका की कुटिया, चैरी का बागीचा , मां जैसी अमर कृतियों के साथ ही उन्होंने सैक्सटन ब्लैक सीरीज और सर आर्थर कानन डायल के जासूसी उपन्यासों और उन जमानों में सनसनीखेज और बोल्ड समझे जाने वाले लंदन रहस्य जैसी जाने कितनी कृतियां पढ रखी थीं। देवकीनंदन-दुर्गाप्रसाद खत्री, प्रेमचंद, गोपालराम गहमरी और मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी के और रवीन्द्रनाथ तथा शरतचन्द्र बंगला के उनके प्रिय लेखक थे। उस काल तक पिता सहित प्रियहरि के परिवार में कोई सदस्य ऐसा न था जिसने चौथी-पांचवी के आगे की शिक्षा पाई हो लेकिन यह विचित्र था कि दिन हो या रात पूरे परिवार में पढ ने और जो पढा उसपर चर्चा की धुंआंधार लत समाई हुई थी। दरअसल यही वे अवगुण थे जिसके कारण प्रियहरि के पिता को उस घर से निष्काषित किया गया था, जहां जैसा कि चर्चाओं में सुनने मिलता था, पैसे गिनने की बजाय पायली से मापकर धर दिये जाते थे। छोटी उमर में ही शादी का तब रिवाज था। ऐसे में कमा-धमाकर पैसा बनाने की जगह जमापूंजी के फूंकने को तब आवारागर्दी के सिवाय और क्या कहा जा सकता था ? तब भी पिता अपने में संतुष्ट रहा करते थे। वे स्वाभिमानी और तुनकमिजाज थे। अपनी जिन्दगी में उन्हे किसी का हस्तक्षेप पसन्द न था।
प्रियहरि को बताया गया था कि पिता को आजादी के आंदोलन के दौर में ही नाटकों का भी खूब शौक था। वे पढ़ने के अलावा खुद लिखते भी थे। नाटकों का शौक इतना बढ चला था कि उन जमानों में बाहर से तीन हजार रूपयों के कर्ज से एक नाटक मंडली बना रखी थी। जमाना पारसी थिएटर और मुक्के सिनेमा का था। पिता उन्हें बताया करते कि किस तरह थिएटर में परदे पर किस तरह चित्र एक-एक कर प्रकट होते और किस तरह सिनेमा का मालिक बाबूलाल खुद हाथ में लंबी छडी लिये तस्वीर में अंकित दृश्य की व्याख्या करता समझाता था। पिता भी आजादी के मसलों पर पारसी थिएटर की छौंक के साथ नाटक तैयार करते और उन्हें शहर में और दूर-दराज जगहों पर कभी खुले में और कभी सिनेमा-थिएटर किराए पर ले खेला करते थे। कभी एक बार तो थिएटर में ठीक प्रस्तुति के वक्त कलेक्टर का फरमान आ पहुचा था कि नाटक में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बातें हैं इसलिए नाटक पर पाबन्दी लगाई जाती है। मौज में वे खुद बुढापे से ढल चुकी आवाज में कभी-कभी अपने नाटकों के गीत जब परिवार के बच्चों को सुनाते तो सब हंस पडा करते थे।
प्रियहरि सोच रहा था कि क्या वे पिता के ही गुणावगुण थे जिनको उत्तराधिकार में पाकर वह दुनियादारी से लापरवाह फिलासफर हुआ चला गया था। वैसा न था तो क्यों उसने गरीबी के संघर्षों के बीच पाई वह नौकरी छोड दी, जिसे पाने लोग पैसा देते एडि यां रगडा करते थे ? उसकी स्मृतियों में सारे चित्र तैर रहे थे।
बाहर का सच गुजर जाता है, अंदर का सच फिर भी रहा आता है । स्त्री-पुरुष का प्रेम और रतिक्रिया समाज में कभी भी वैध माने गये हों, ऐसा मैने नहीं सुना । रतिक्रिया का नियमन विवाह की संस्था ने दांपत्य ने समाज में कर जरूर दिया है लेकिन विवाह में प्रेम की चर्चा कभी नहीं हुई । प्यार हमेशा बंधनों को फांदने की कोशिश करता रहा है और फांदकर ही होता है । संचित यौनरति जब किसी विपरीतलिंगी पर चित्त में केन्द्रित हो जाती है तब वह प्यार हो जाता है । सामान्य यौनरति केवल यौन की चाहत है और प्यार उसका विशेषीकृत रूप । यह ग़ौरतलब है कि प्यार भी तब तक ही प्यार रहा आता है जब तक वह रतिक्रिया की अतृप्त प्यास है । प्यास बुझाने की रूकावटें खत्म हुई नहीं कि सारा कुछ खो जाता है । प्रेम में भी विवाह का पड़ाव ऐसा ही मोड़ हैं । ऐसा क्यों होना चाहिये ? इसके पीछे शायद अस्तित्व और वरण की स्वतंत्रता को बनाये रखने का मनोविज्ञान है ।
यौनरति की चाहत मनुष्य के जन्म के साथ ही जुडी होती है । यौनांग छिपाये जाने की चीज है, उसकी चर्चा, प्रदर्शन, क्रिया वर्जित समझे जाते हैं । शायद इसीलिये वही बच्चे को तभी से लुभाने लगता है जब उसकी चेतना यौनांग को महसूस करने लगती है । तीन-चार साल की उम्र से ही यह महसूसना शुरू हो जाता है । तब एक ओर वर्जनायें होती है और दूसरी ओर वर्जनाओं को तोडने के लिये एकान्त और साथ की तीव्र कामना से भरी कोशिशों को आरंभ होती है । यह कामना इतनी तीव्र होती है कि जहां से भी निकल भागने की संधि हो चाहे वह नर हो या नारी मनुष्य का चित्त निकल भागता है । कामना की तृप्ति के लिये साथी की चाहत फिर जीवनभर चलने वाली चित्त की प्रक्रिया बन जाती है । ऐसी प्रक्रिया जो बाहर से आवृत्त अंदर की इतनी और ऐसी दिशाओं में ले जाती है कि मनुष्य का सारा जीवन उससे परछाई की तरह परिचालित होता है । यह वह अदृश्य है, जो कभी कभी तो समाज की सारी वर्जनाओं को तोड विस्फुटित होता है । अवसाद से अपराध तक के दायरे इसमें सम्मिलित होते हैं । घर से भाग जाना, आत्महत्या, बलात्कार, हत्या और अन्यथा सारी कुंठायें इसी से जन्म लेती है ।
हम लोगों का घरोबा का था । हम यानी मेरा साधारण मध्यमवर्गीय घर और हम की वह, यानी उसका घर साहूकार का हवेलीनुमा दो मंजिला बडी-बडी कोठरियों और पचीसों कमरों वाला बहुत बडा घर । ऊपर एक ओर उनका रहवास, बीच में विशाल आंगन और इसके इर्द-गिर्द बडी बडी कोठरियां जिनमें उनके बड़े किराना व्यापार के सामान्य अनाज नारियल वगैरह की सैकडों बोरियां, बांस के बड़े-बड़े पिटारे जिनमें न जाने क्या सामान आता था । बडे-बडे कार्टन्स उनमें ठंसे रहते थे । आंगन और वे नीम-अंधेरी कोठरियां इस घर के चंद बड़ों के बाद बच रहे बच्चों के लिये लुका-छिपाई खेलने ओैर जिज्ञासाओं को खोलने के काम आती थी । उन दिनों बिजली उस कस्बे तक नहीं पहुंची थे हम छोटे थे । छोटों में कुछ बड़े। उसका नाम कावेरी था । घर की छोटी लडकी। उसकी 14-15 साल की उम्र थी । विशाल आंगन में इधर उधर कुदराते और कोठरियों में छिपते बच्चों के साथ हम दोनों भी खिलाड़ी और दर्शक थे । कभी-कभी ऐसे मौके आते जब पाया जाता कि नीम अंधेरे कोने में खेलते नन्हों के मुन्ने हाफपैंट से बाहर है और वे उसे टुन्न-टुन्न बजाने तान रहे हैं । एक खिलंदड़ी हंसी होठों पर तैरती और कावेरी डांटती - ''छिः ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं ।''
यह साधारण अनुभव था । वैसा होता ही था ।इसी माहौल में साल दो साल गुजर चले । मैं उससे छोटा था, वह बड़ी। वह मकान जितना विशाल था उसके लिये वहां खेलते बच्चे हम कम थे । बच्चे तीन-चार-पांच वगैरह और कमरे कोठरियां उनके लिये अनंत । बाहर दूकान में नौकर व्यस्त होते । कुछ बच्चे बाहर सड़कों पर खेलते और कुछ दो तीन लुकी-छिपी में अंदर व्यस्त । एक दिन हमने पाया कि आंगन के कोने नीम अंधेरी कोठरी के पास टिका पिटारा हिल रहा है । कावेरी की नजर पडी बोली चलो देखते है क्या है। निहायत दुबली-पतली और सांवली कावेरी चंचल थी । साहूकार की लडकी थी इसलिये मेरी लीडर वही थी । हमने बारीक छिद्रों से झांकने की कोशिश की । दिखाई तो पडा नहीं आवाजें सुनीं । दूध की मलाई लगाने में बहुत अच्छा लगता है - एक स्वर । मुझे मालूम है तुम्हें दूध पसंद है । इसीलिये आज मैं मलार्इ्र लगाकर आया हूं - दूसरा स्वर । कावेरी ने होठों पर एक अंगुली टिकाई और मेरी आंखों में झांकते चुप रहने का संकेत किया । उसने एक ओर से उस जादूगर के विशाल पिटारेनुमा झांपी का ढक्कन उठाया । हम दोनों ने देखा बाबू और लक्खू के नन्हें अपना टुन्न लहरा रहे हैं । बाबू का हाथ लक्खू के कंपित पर था और लक्खू मलाई की चिकनाई से चकते बाबू के कंपित की घुंडी निगलते होंठ चला रहा है ।
मेरा दिल अचानक थमने लगा । वह ठहराव दिल की धडकनों से तेज होने के पहले का था । इस बार मैने कावेरी की आंखें में देखा और होठों पर अंगुंली टिकाते चुप रहने का संकेत किया । झांपी के अंदर बच्चे अपने आप में इस कदर तल्लीन थे कि हमने कब झांपी खोली और बंद किया उन्हें पता ही नहीं चला । कावेरी ने मेरा हाथ पकडकर खींचा और बोली -चलो अपन भी लुका छिपी खेलते है ।
वह दौड़कर परले किनारे की नीम अंधरेी कोठरी में जा छिपी । रोशनी की छाया उन कोठरियों में दरवाजे के इर्द-गिर्द ही रहती थी । शेष रहा आता बोरियों में छिपा अंधेरा । मै उसके पीछे भागा । बोरियों के ऊंचे-नीचे ढेर पर अंधेरे में मेरी नजरें कावेरी को टटोल रही थी । अचानक एक जगह सरसराहट हुई । धीरे-धीरे अंदाज से मैने बोरों की पहाडियों में वह घाटी ढूंढी जहां कावेरी छिपी थी । पास आने पर उसने और दुबकने की कोशिश की मैं पहुंचा तो उस संकरी जगह में उभरे बोरे से टकरा ठीक उसके ऊपर गिरा । दोनों का उठना मुश्किल था । उठने संभलने की कोशिश में कावेरी का बदन मुझसे और चिपका पड रहा था । लुका-छिपी का खेल कब दूसरे खेल में बदल गया इसका पता ही नहीं चला । दोनों की सांसें भारी हुई जा रही थी । मेरी छाती से कावेरी की छाती दबी पड रही थी । जंघाओं के बीच का लंब फन काढे लपका जा रहा था । कावेरी फुसफुसाई - अच्छा लग रहा है,, दिखाओ । जाहिर है ऐंठते लंब की कमर पर चुभन को उसने महसूस कर लिया था । मैं ढीली ढाली हाफ पैंट पहनता था और कावेरी वैसी ही फ़्राक में थी । उसने मेरे कंपित लंब को पकडा और नीम अंधेरे में निहारती बोली आह बडा अच्छा है । कावेरी ने मेरी गोद में सिर झुका कंपित लंब की घुंडी होठों के बीच निगलते पूछा – मैं भी देखूं भला कैसा लगता है । मेरी अधीरता वह बढाये जा रही थी । उसके होठों को निगलता मैने उसे वहीं दबाया और बोरों की गडमड्ड उभार के बीच उभरे उसकी नन्हीं के बीच अपनी काया के विस्तार को डुबा दिया । बच्चों के अपने हाथों गुदगुदाये जाने वाला वह मांसल विस्तार उस रोज पहली बार कहीं और कसरत करता गुदगुदा रहा था ।
''हाय रे कितना अच्छा लग रहा है'' - कावेरी बुदबुदाई । अधिक कौशल की गुंजाइश न थी। चंद मिनटों में यौवन के रस से हम दोनों के नन्हा-नन्हीं नहा गये थे । फिर कुछ देर खामोशी रही । ऐसा लगा जैसे दोनों को नींद आ चली हो । कावेरी ही बोली -चल उठ चलते है । मुझे चिपकाती और मेरा चुम्मा लेती उसने कही -
तू बहुत अच्छा है । आज मुझको पहली बार मजा आया । अब अपन रोज यूं ही खेलेंगे, हां। उसने हिदायत दी कि ये बात किसी को बतानी नहीं है ।
यह भांपते हुये कि इर्द-गिर्द आवाजाही तो नहीं है । हम बाहर निकल आये । दोपहर होने को आई थी और भूख का समय था । आंगन में पडी झांपी अब भी पडी थी । कावेरी ने ढक्कन उठाया । दोनों नन्हें खरगोश झांपी से कुलांच चुके थे । उस दिन के बाद कावेरी ने पिटारियों में झांकना छोड दिया था ।
झांपियों और अंधेरे खंडहरों के वे दिन समूचे बचपन में फैले हुये थे । गर्मियों में जब बडे बुजुर्ग घर की छांह में राहत ढूंढते थे । तब नन्हें हम लोग मिट्टी के खंडहरों में लुका छिपी खोलते थे । उस लुका छिपी के अंधेरों में एक एक दो-दो कर अंधेरे कोनों में साथ होना भी अजीब गुदगुदी भरा होता था । खंडहर का अंधेरा सूना एकांत बदन के अंधेरे में छिपे उपेक्षित से दोस्ती करने और खेलने की चाह जगाता था। उस उपेक्षित का ,जिसकी तरफ उजाले और स्वीकृत रिश्तों की भीड में भूले से भी देखना गुनाह था। कभी बडे लौंडों के समूह में होते थे तो वे अजीब तरह के खेल सिखाते । खंडहरों के बडे ढूह में इमली का एक विशाल दरख़्त था । चूडीहार मुसलमानों की बकरियां वहां मिमियाती चरती और खेलती थीं । एकाध दफे यूं हुआ कि बड़ी उम्र के शैतान लौंडे वहां हमारी अगुवाई में पड गये । बारी-बारी से वे छोटों को चुनते और पुटठों के बीच चढ़ने का खेल सिखाते . आनाकानी करने पर वे डांटते और मजा लेते । पशोपेश में पड़े छोटे उनकी आज्ञा का पालन करते करते डर से भाग खडे होते थे । आबादी तब कम हुआ करती थी । बस्ती से बाहर एक डेढ़ कोस में ही जंगल शुरू होता था । आंवलों के खूब पेड़ हुआ करते । भरी दुपहरी पत्थर मार-मार आंवले झड़ाते और जंगल की झुरमुटों को लांघ आध एक मील दूर घुसकर वहां के शांत सन्नाटे को धुकधुकी में महसूसते खड्डों, नालों, जानवरों से आशंकित खौफ खाते सांझ ढले तक लौट आते थे । उन दिनों यही हमारी पिकनिक का खेल था । बच्चे के उस मुकाम तक बड़ा हो चुकने के बाद, जहां उसकी देह का गोपन अपने स्वर्गिक रस का अहसास कराता, बच्चे में निषिद्ध कामनाओं की चुलबुलाहट पैदा करता आदम के बाग में विचरण की उत्कट प्रेरणा जगा देता है, उसके सामने दो ही बातें रह जाती हैं। एक वह, जिसमें वह स्वयं को पाता है और दूसरी वह, जो उसे निरन्तर खींचती आदम के बाग की सैर कराने लुभाती है। वह उमर ऐसी ही थी । औरतों-लडकियों की दुनिया उन दिनों चहारदीवारियों की ही हुआ करती थी । इसलिये उनकी तरफ ध्यान चढ़ती उमर के साथ ही जाना शुरू हुआ था । आम तौर पर छोकरों के समूह में छोकरे ही यार हुआ करते थे। आकर्षण का सूत्र क्या है, उसके नियम क्या हैं, यह कहना मुश्किल है । समवयस्कता में साथ चिपकने का लगाव और उसकी चाहत समानधर्मिता से पैदा होते थे । कुछ साथी ऐसे ही हुआ करते थे । रमण हकलाता था लेकिन सीधा और कुशाग्र था । उससे मेरी दोस्ती थी । सभी उसके इर्द गिर्द रहते थे । उन दिनों तो वैसे चिपकने-चिपकाने की जुगुप्सा केवल गुदगुदी में थी, लेकिन सालों बाद बड़े जवान हो जब हम नौकरियों में थे और आगे बढने की जुगत में एक बार संयोग से साथ किसी नगर में मिले तो उसे मैने अपनी पुरानी यादें जगाने अपने ही साथ ठहरा लिया था । खूब यादें दुहरायी गयी । मेरी कोठरी के एकांत में जब रात गहराने लगी तो माहौल भी जवानी की बातों का चल पडा । साथ सोने में हम दोनों झिझक गये इसलिये मापन की गोपन जिज्ञासा बातों और बातों सी बातों में सिमट आई । हम दोनों का ध्यान एक दूसरे के परम गोपनीय पुरुष दंड पर केन्द्रित हो गया था । उतावले पथ में सनसनाता अपना गोपन पौरुष मैने प्रकट किया और उससे कहा कि स्पर्श कर वह जांचे कि कैसा है ? उसका गोपन पौरुष जब मैने देखना चाहा तो बडे संकोच मे पड़ता वह राजी हुआ । उसने निकाला और मैने उसे जांचा । वह बोला कुछ नहीं बे, एक जैसे ही हैं । तेरा पुरुषत्व कुछ ज्यादा मोटा है । मेरा कुछ लंबा लेकिन पतला है । इस सब के बावजूद हमने वैसा कुछ नही किया, जैसा बचपन में खेल-खेल में हो जाया करता था । प्रायः वैसा खेल संकोच-भरा और एकांतिक हुआ करता है। बहुत छोटी अवस्था में ही घर से हास्टलनुमा जगह में बहिष्कृत मुझे उस मौज का भी अनुभव हो चला था ।