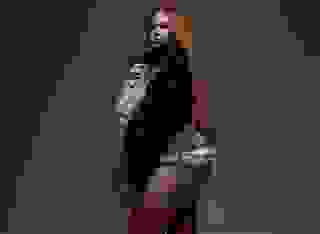Note: You can change font size, font face, and turn on dark mode by clicking the "A" icon tab in the Story Info Box.
You can temporarily switch back to a Classic Literotica® experience during our ongoing public Beta testing. Please consider leaving feedback on issues you experience or suggest improvements.
Click hereवहां हम लोग गिनकर कुल दस थे । खाना-पीना,, रहना, पढना, स्कूल जाना सब नियमित और समान था । हम अलग अलग पृष्ठभूमियों से आये थे । तीसरी-चौथी से आठवीं-नवीं के बीच के विद्यार्थी थे। भोजन के समय शुरू-शुरू में ''सहनाववति, सहनौ भुनक्ति, सहवीर्यम् करवावहे'' का मंत्र हम पढते थे। बाद में मंत्र तो छूट गया और सहकार में केवल भावना रही आई थी ।
एक कमरे में लाइन से चार-पांच खाटें पडती थी । कभी-कभी पढते-लिखते मौज का माहौल बनता । वैसे माहौल का खास मजा तब बनता जब कुछ और साथियों की गैरहाजिरी होती और कमरा दो या चार के लिये रातों को हमारे बीच छोड जाता । सच होता या झूठ जानने का जरिया नहीं था लेकिन गांव के वे लडके देहात की ''ऐपन आड़ लिलार'' छोकरियों के किस्से छेडते और लिजलिजे चुटकले सुनाते थे। एक ने किस्सा सुनाया कि कोई गांव की लडकी थी । अपनी दादी के साथ रहती थी । बरसात के दिन लग रहे थे । पास का झडीराम बगल की अंधेरी कोठरी में गांव की उस लडकी के पीछे लगा था । बुढिया थी बगल की कोठरी में । झडीराम जब ललना की झाडियों में प्रवेश करने दंड संभाले आगे बढने लगा तो आधे भय और आधे लोभ से गदगदाई गांव की लडकी वह ललना चीखी -'' देख न दाई झडी हर करत हे मै का करों ।''
दाई ने अपनी अंधेरी कोठरी से ही जवाब दिया- ''बने हे फुलमत करन दे झडी लगही तभे तौ बनही बेटी ।'' उसका आशय वर्षा की झड़ी से था।
गांव की उस ललना ने उसमें मनचाहा आशय ढूंढ लिया था। उसने जवाब दिया
-‘ जा अब तंही कहत हस तो महूं कुछु नइ करंव।‘ बुढिया का जवाब उसके लिये स्वीकृति का बहाना था । उसने झडी को संभाला और जमकर बरसात करा अपनी सारी जमीन भिगो ली ।
पहाड़ों के उस हास्टल का संबंध एक परमार्थ संस्था से था । देखभाल एक बाबाजी वैद्यराज करते थे । उनकी एक नजदीकी मरीज दवाखानों के अंदरूनी हिस्से में उनसे परीक्षण करा ऐसी तसल्ली पा चुकी थी कि उन प्रौढ़ वैद्यराज की कोठरी में सूनी दोपहरियों में अपना इलाज कराने वह यूं घुस पड़ती थी कि बाबाजी भी धीरे-धीरे उसके मरीज हो गये थे । यह ऐसा मर्ज था कि मरीज ही मरीज का इलाज कर सकता था । कई बार कौतुक में परिसर के विशाल बागीचे में यहां वहां पेडों के पीछे छिपे हम छोकरे दो मरीजों के मिलन और इलाज की जासूसी में लग जाते थे ।
त्यौहारों की या गर्मी की छुटि्टयों में ऐसी रातें भी आती जब कमरे में एक दो तीन खाटें ही आबाद होती थीं । मैत्री के संबंधों में नजदीकी गहराती चली गई थी । साल दर साल गुजर चले थे । इसलिये दूरियां भाग गई थी । रात यूं लगता कि दूर-दूर क्यों सोया जाये । तब एक के इशारे से दूसरा पास की खाट में आ जाता । बातों ही बातों में दूसरी खाट कब गायब हो जाती पता न चलता । फिर देहों का साथ अंगों में सनसनी भरता दंड को दंड-बैठक कराने लगता। किशोरों के अन्दर से बाहर कुलांचते उनके वे खुलकर कब लिपटते-झपटते आपस में नाप जोख करने और टकराने लगते इसका पता ही न चलता था। पिछवाडा कभी किशोर दिमाग में घुसता न था इसीलिये अंततः एक दूसरे का हाथ मदद में सामने आता और ढेर सारी झाग उगलते उन्हे शांत कर जाते थे। एक-दूसरे को देखने की जिज्ञासा हर किसी के मन में रहती थी।और यूं फिर सब ने धीरे-धीरे सब को जान लिया था । हममें से एक था मनीराम, दुबला पतला, पक्की काली रंगत का किशोर । लेकिन उसकी सरलता और स्वभाव सभी को पसंद थे । था तो मनीराम साधारण ही कद का हमीं लोगों जैसा । बल्कि कुछ छोटे ही कद का, लेकिन गहरे श्याम रंग के चिकने चेहरे वाले मनीराम का अंदर वहां सभी को लुभाता था । वहां भी गहरी श्यामता थी, लेकिन पूरी चिकनाई के साथ । यह विचित्र था कि छोटे कद के सुकुमार मनीराम का अंदरूनी मनीराम औरों से लंबा और लुभवना था । वह सर्वविदित हो गया था । यहां तक कि उस पंद्रह एकड़ में फैले बागीचे से युक्त हास्टल का नेपाली माली सह चौकीदार भी जो उम्र में हम लोगों से बहुत बडा और जवान था स्पृहा में आश्चर्य करता और बोल उठता - ओरे बाबा रे मैने देखा है मनीराम को। वह तो लंबा है, जोरदार है ।
बाबा वैद्य तो क्या वहां का चौकीदार, वहां का रसोइया जो बदलते रहते थे, सभी अपने-अपने ढंग से चालाक थे । बाहर से नौकरानियां काम करने आती और धीरे-धीरे यूं होता कि इन सब के तनावों को राहत देने का काम निबटा जाती थी । एक लडका था पूरनदास । उसके बारे में चौकीदार ने कभी यह जाना और फैलाया कि किसी दिन पूरनदास ने विशाल लंबाई में पसरे कमरों के छोर पसरी सीढ़ी पर उस परिसर में रिरियाती कुतिया से पश्चालिंगन में अपना प्रेम दर्शा डाला था । किसी और एक दिन बताया गया कि सुबह-सुबह रसोई या में रसोई बनाते रंगीन मिजाज रसोइये खोरबहरा ने अंदर पुताई करने गई नमकीन रेजा मजदूरनी के साथ गुप्त रसोई भी पका डाली थी । बहाना यह था कि ठीक दरवाजे के ऊपर दीवार पोतनी थी सो सीढ़ी टिकाने और सहारा देने उसने रसोई का दरवाजा बंद कर लिया था । वह हाफ पेंट पहनता था । रेजा की पुताई करने में उसे परेशानी नहीं हुई होगी ।
दिन और रात गुजरते दस में से सात-आठ फेल या पास होकर या दीगर पारिवारिक दबावों से हास्टल छोड चुके थे । उमर के बढ़ते-बढ़ते रुचियों और संगत में भी बदलाव आ गया था । यहां एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी थी, जहां बैठकर मैं सारे अखबार और पत्रिकायें माया, मनोरमा, मनमोहन, मनोहर कहानियां, धर्मयुग, हिन्दुस्तान वगैरह चाट जाया करता था । वह सब तो सुबह शाम का दो दो घंटे का दिमागी नाश्ता था । दिमाग का पेट न भरता तो सेक्स, बच्चों के सीरीज के उपन्यास, कुशवाहा कांत की किताबें, बाल्ज़क, शरतचंद्र, रवीन्द्र, बंकिम, यशपाल, भगवतीचरण वर्मा, गुरूदत्त वगैरह के उपन्यासों से दिमाग को तंदुरूस्त करता । सेहत को अंगूठा दिखाता मैं समय बिताता था । चर्चाओं में अब प्रौढ़ता थी और स्कूल के दूसरे दोस्त साथ बैठने लगे थे ।
एक था आनंद । वह स्कूल के खुलने और बंद होने के बाद किसी दुबली, सांवली रेशमा के दीदार से आंखे सेंकता था । मेरी पसंद सरोजनी थी, दुबली-पतली सुतवां देहयष्टि की गंभीर गोरी छोकरी । हम दोनों अपनी अपनी पसंद की यादों में कसीदें काढते कविता, कहानी की उधेडबुन में रहते गो कि वह उस समय हमारे बस के बाहर की चीज थी । पहाड़ी कस्बे के एकमात्र सिनेमाघर के बगल में वह रहता था और फिल्मों के टुकड़ों को कांच के लैन्स से सिनेमा की तरह फैलाकर देखने का शगल वह रखता था । तीन-चार मील के दायरे में और सात-आठ हजार की आबादी के कस्बे में वह सिनेमा रोज शाम बगैर घडी घंटाघर का काम करता था । पूरे शहर में वहां बज रहे ग्रामोफोन ही आवाज गूंजती थी । बाहर लाउडस्पीकर और रेडियो का चलन भी बहुत कम था इसलिये ''अंखिया मिलाके नजरें चुराके, एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन, सांझ ढले खिडकी तले तुम सीटी बजाना छोड दो,'' वगैरह की तरंग से क्रस्बे का मौसम भी रोमानी हो जाता था । लोग समझ जाते कि शुरूवात छः बजे से हुई है । ठीक साढे-छः बजे जब ''आरती करो हर हर की करो, नटवर की, भोले शंकर की'' वाली धुन बजती तो पता लग जाता कि सिनेमा शुरू हो रहा है । नाडिया-जानकावस, जयराज, निरूपाराय, भगवान और मुकरी की फिल्में आती जाती रहती । दिलीपकुमार देवानंद, अशोक कुमार, राजकपूर जैसे बडे कलाकारों की या जैमिनी, महबूब सोहराब मोदी, फिल्मिस्तान की फिल्में महीनों के पोस्टर प्रचार के बाद जब आती तो लोग बा-कायदा घरों में सिनेमा देखने के कार्यक्रम बनाते अपनी रोजमर्रा की सारणी को योजनापूर्वक तब्दील करते थें । वह उत्सव की तरह हुआ करता था ।
मदर इंडिया, मुगले आजम, कोहिनूर, जंगली, गंगा जमुना, जिस देश में गंगा बहती है, तुमसा नही देंखा के जमाने तक मेरी स्कूलिंग खत्म हो चली थी और चर्राती जवानी अब नये सपने देखने लगी थी । ये वे दिन थे जब पंडित नेहरू, लोहिया और चीन भारत पर छाये थे । नेफा की वारदात गर्म हो रही थी ओर कृष्ण मेनन का जादू गायब हो रहा था । इस समय तक प्रकाशित सारा चर्चित साहित्य मैं पढ चुका था । यशपाल का झूठा-सच, ताराशंकर का गणदेवता, विभूतिभूषण का पाथेर पांचाली, आरण्यक, और ढेर सारा साहित्य मैं दिन-दिन पढ़ता बैठता । बचा समय आवारागर्दी और सिनेमा देखने में गुजरता । यह दौर मेरे पुष्पा युग में प्रवेश का था । नवीं दसवीं में पढ़ने वाली यह छोकरी ठीक सामने के मकान में थी । पहाड़ी गोरी रंगत लेकिन आंचलिक हिन्दी का परिवेश । चेहरा उसका अंडाकार था, सिर से चिपटी घुंघराली जुल्फें, बडी बडी आंखें और अल्हड अदायें ।
लडकों के समूह में कद काठी में असाधारण होकर भी मैं प्रखर था । पुष्पा से देखा-देखी की शुरुवात एक अनोखे अंदाज में हुई । आंखें जब-तब मिलती थीं और आंखों के इस मिलन में एक दूसरे की गतिविधियों को चाहत के साथ देखने का लगाव जाहिर है हम दोनों में छिपा था । एक रोज मै अपने दो मंजिले पुराने ढब के बाडे के दरवाजे सामने नल के कटघरे में बैठा था । आसपास छोकरे खेल रहे थे । कोई ऐसी बात हुई कि हमारी आंखें मिली, चमकीं और पुष्पा के होंठों को उसकी आंखों की संगत में मैने चुहल से हंसते चेहरे के साथ हंसता देख लिया । दिलों के तार खनखना रहे थे । मेरी आंखों ने उसे बरजा और मेरे नल की सपाट दीवार पर मेरे हाथों ने लिख दिया हंसों मत । वह और मुस्कुराई और हंसी । मैने वैसा इसलिये लिखा था कि आंखों से आंखों की मुठभेड़ लोगों की आंखों में न आये । बस क्या था संकेतों की भाषा पर सहमति और मौज का मूड बदलकर इश्क में तबदील हो गया । मेरे दो मंजिले की खिड़की से उसके दरवाजे की सीढ़ी दिखाई पडती थी जहां वह बैठ जाती थी । देखा-देखी का बुखार सर पर इस कदर चढा कि सम्मिलन और सहभोग की चाहत बेचैन करने लगी । घंटों की टकटकी और मौन संवाद । उन जमानों में अवसरों की छूट ज्यादा न थी तो प्रेम उसकी प्यास में होता था । बल्कि सच तो यह है कि अब भी प्यास ही प्रेम है । प्यास बुझी कि प्रेम खतम । इसीलिये अब तो स्कूल के छोकरे-छोकरियों के बीच खुली बातचीत का माहौल और मोबाइल फोन ने प्यार को पेप्सी बना लिया है । इंस्टेंट प्यार, इन्स्टेंट संभोग । देवदास की कथा दोहराने यहां कोई अवकाश नहीं है । औरतें मर्द की कमजोरी और अपनी कीमत जानती हैं। इसलिये अब हो तो यहां तक चला है कि मजबूर औरतों ने ही नहीं, बल्कि भद्र श्रेणी की छोरियों और औरतों ने मर्द की मजबूरी को मनोरंजन और पैसा कमाने का धंधा बना लिया है ।
किशोरी पुष्पा से मेरे किशोर ह्रदय का इश्क साल-डेढ़ साल चला। लेकिन माजरा वही था। ''सब कुछ सौंपना, लेकिन ताला न खोलना'' की नैतिकता आड़े आती थी। कमला मेरी पड़ोसन थी, तकरीबन हमउम्र गदराया श रीर। कमला से मैंने चिट्ठी भिजवाई कि मेरा प्यार पुष्पा कुबूल करती है फिर मिलने से क्यों कतराती है ?''
कमला चिट्ठी के साथ ही चिट्ठी का जुबानी जवाब लाई'-''वो कहती है कि नहीं। वह काम संभव नहीं।''
उतावला होता मैं धीरे-धीरे बहुत अधीर हो चला। सरे आम पुष्पा को छेड़ना, मोहल्लों में ट्यूशन पर जाते उसमें जूड़े से फूल खींच लेना, फिकरे कसना, उसके घर में सीकचों के पार कंकड़ में फंसाकर मोहब्बत के पुरजे फेंकना वगैरह। होली में मैंने सरे आम उसे छेड़ते उसके गालों पर रंग पोत दिया। अपनी समझ में दीवानगी के वैसे इजहार से मैं हीरो बना जा रहा था। मुझे क्या मालूम था कि औरत की निगाह में प्यार बंधनों और पोशीदगी में होता है। उस पर हक जताना और सरेराह दावा ठोकना स्त्री की निगाह में अभद्रता और गुंडागर्दी होते हैं। पुष्पा मुझ पर नाराज़ हुई और यूं रूठी कि बाद का बड़ा अरसा मेरे लिए मायूसी और उदासी का रहा आया। बाद में आवारागर्द और गैर-जिम्मेदार होने से बचाने मुझे कहीं और दूर भेज दिया गया। पुष्पा कहां गई, कहां है फिर मैंने नहीं जाना। यह कैशोर्य का वह दौर था जवां चढ़ती उमर उस बछड़े की होती है जो चढ़ तो नहीं पाता लेकिन चढ़ने की उतावली भरी कोशिश जरूर करता है।
पुष्पा से संबंधों-असंबंधों का दौर बीतते-बीतते ही मेरी निकटता आरसी से हो लगी थी। किशोर-वय बड़ी अजीब होती हैं। प्यार-व्यार तो जो कुछ होता हो, एक किस्म की चंचल उतावली और खिलंदड़ापन ज्यादा होता है। भविष्य के जीवन की सच्चाइयों और उतार-चढ़ाव का तब वैसा ध्यान नहीं होता है जैसा प्रौढ़ होते-होते आदमी अनुभव इतना है। आरसी और मेरी उम्र में तकरीबन तीन साल का फर्क था। उसे मुझसे उम्र में काफी बड़ा मेरा रहनुमा दोस्त ब्याह कर लाया था। दोस्त की उमर अगर पच्चीस थी तो मेरी सत्रह और आरसी की बीस। वह उस शहर में अकेला था। हालांकि मैं चंचल और आवारागर्द समझा जाता था, पढ़ने-लिखने की गंभीर रुचियों में हममें दोस्ती पैदा कर ही थी। राजनीति, साहित्य और दीगर ज्ञान-विज्ञान के मामलों में हम दोनो में खूब चर्चा होती। दोस्त और आरसी के सामने मैं बस बच्चा ही था। मैं अक्सर उन्हीं के यहां रहा आता था। अंदर किशोर सुलभ जिज्ञासाएं थीं, ज्ञान-विज्ञान के लिए भी और लुगाई स्त्री-देह के प्रति भी। बड़ा देखने की कोशिश करने पर भी काया और व्यवहार में ऐसा बचपना था कि मैं युवा या युवा जैसा बड़ा समझा जाने के काबिल उनकी निगाह में न था। दोस्त की गैरहाजिरी में भी बातें करना-गप्पें लड़ाना और छोटे-मोटे कामों में हाथ बटाना, सौदा सुलफ पास की दूकानों से लाना-लेजाना में अपने दोस्त और आरसी का लगभग प्रिय अनुचर ही था। मैं खुद भी अपनी उस हैसियत से खुश था। न जने क्यों बहुत दिनों तक अन्यथा कोई बात मेरे चित्त में आई भी नहीं।
आरसी आई तो देहात के किसी बड़े घर से ही थी, लेकिन अनिन्द्य सुन्दरी थी।बेदाग गुलाबी चमक और सुचिकरण देहयष्टि के हाथ उसकी जवानी कैशोर्य से आगे बढ़ चली थी यद्यपि अपने सहज स्वभाव और ग्रामीण संस्कारों के चलते शहर में होने के बावजूद उसके व्यवहार में किशोरपन ही छलकता था। मेरे दोस्त पति की तरह ही उस आरसी में भी खुलापन और निश्छलता थी। उसका खूबसूरत चौकोर चेहरा भरा-भरा था। आंखें अपनी चमकती भूरी पुतलियों की लुभावनी चमक के साथ बड़ी-बड़ी थीं। मुलायम गुलाबी होठों के बीच उसकी झक्क सफेद दंतावली जैसे समानुपातिकता में यत्न से तराशी गई थी। जब वह सहज मुस्कुराहटनुमा हंसी हंसती तो विस्तरित गुलाबी होठो के बीच उसकी दंतावली की चमक उसकी अनगढ़ सुरीली आवाज की खनक के साथ बिजली की चकाचौंध पैदा करती थी।उसके वक्ष पुष्ट थे और चोलियों के बीच कुंभों की तरह उभरे दिखाई पड़ते थे। साधारण औरतों में ब्रा का चलन बाद में धीरे-धीरे हुआ था लेकिन बगैर ब्रा के भी चोली के कसाव में स्तनों की नुकीली घुंडियां स्पष्ट दिखाई पड़ती थीं। चेहरा ही नहीं, आरसी नख से शिख तक कोमल बदन की तराशी जीती-जागती गुड़िया की तरह थी। उसकी केश-राशि घनी थी। काली घटा की तरह सघन केश-राशि अपनी हल्की सलवटों के साथ घुंघरालेपन का आभास देती और सिर से पीठ पर लहराती कटिप्रदेश के नीचे तक उसकी अयत्नज देहाती चोटी के रूप में फैली झूलती रहती थी। यह अजीब बात थी कि किशोरी कामिनियों के प्रति ललक भरी चाहत के बावजूद मेरा ध्यान बहुत अधिक अपने ठीक करीब खेलती इस खूबसूरत आवाज गुड़िया पर नहीं गया था। सहज परिवार जैसे आपस के संबंधो और विवाहिता की हैसियत के साथ उसके उम्र में बड़े होने के अहसास के चलते शायदवैसा नही हो पाया था। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि पहली बार उस अहसास ने मुझसे प्रवेश किया। बसन्त का मौसम और होली का माहौल था, होली अभी दो-दिन की दूर थी। शाम का समय होने को आया था। जब मैंने उसके घर प्रवेश किया तो वह सफाई के सीमेन्टी चौखटे पर जूठे बर्तन घिस रही थी। मेरी ओर उसकी पीठ थी इसलिए मेरा आना वह देख न पाई थी। अपनी किशोर सुलम चंचलता में दबे पांव पहुंच मैने पीछे से हथेलियां बढ़ा उसकी पलकों पर अंगुलियां रख दीं। आरसी में अल्हड़ खुलापन था। इसलिए हल्के से चौंकने के बावजूद वह भयभीत न हुई। मेरी अंगुलियों को उसने अपनी अंगुलियों के स्पर्श से पहचाना और बोली-'छोड़ो न, मैं बर्तन मांज रही हूं। मेरा नाम उशा रते उसने कहा कि मैं पहचान गई तुम अमुक हो।'' अनौपचारिक संबंधों का माहौल, बसंत का मौसम और उस खास क्षण की रंगत अचानक कुछ ऐसी हो उठी कि उसका गुलाबी चेहरा अपनी अस्तव्यस्त अलकों के साथ किंचित लालिमा से भर गया था। मैंने पलकों पर से अंगुलियां हटा दी थीं । लेकिन अचानक वे लालिमा से सक्रिय हो उसे उसके गालों पर चहलकदमी करने लगीं। उसकी आँखों ने एक बार मुड़कर मुझे निहारा था, लेकिन अवरोध का भाव न तो आंखों में था न मुद्रा में। सफाई की चौखट के लंबे संकरे कोर पर वह बैठी थी इसलिए बदन असंतुलन में लड़खड़ा गया था वह पीछे लुढ़कने जैसी हो रही थी-''छोड़ो न, मैं गिर जाऊंगी -उसने कहा। मेरे घुटनों पर वह थमी थी। गालों से हथेलियां हटीं और न जाने क्या मुझे क्या सूझा कि उसके कमर को दोनो हाथों से घेरते अपनी हथेलियों में उसके गदराए कुम्भों को थामे आगे झुकते हुए उसके गुलाबी होठों पर मैंने अपने होठ रख लिए। सारा कुछ आकस्मिक और अनियोजित था। उसकी सांसों की धड़कनों की तेजी मेरी हथेलियों में फंसे काया- कुंभों के उतार-चढ़ाव से मेरी नसों में पहुंच रही थी। वह कह रही थी-''तुम भी अच्छे हो। कोई देख लेगा तो ! देखो दरवाजा खुला है।''
उस वक्त अचानक मेरे बलात बंधन से मुक्त सामने खड़ी आरसी के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी थी। मैंने देखा कि आरसी के गुलाल मिश्रित दूध जैसी गोरी रंगत का चेहरा अचानक गहरी लालिमा से भर उठा था। कोमलता की जगह वहां जड़ता ने ले ली थी। आरसी की मुद्रा गंभीर हो उठी थी और वाणी मूक हो चली थी। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें लाल होती आंसुओं से डबडबा रही थी। वे मूकता में मुझे घूर रही थीं। मेरा मन तब भय से भर उठा था। इस आशंका से कि वह नाराज न हो उठी हो और कहीं चुगली न कर बैठे मेरा मन घबरा रहा था। जीवन के बाद के पड़ावों में फिर कभी यह ज्ञान हुआ कि वैसी अवस्था स्त्री में नाराजगी में ही नहीं, अपितु वासनाओं से दीप्त देह की संभोगातुर कामना में भी प्रायः प्रकट होती है। ऐसे ही पड़ावों में प्यार की विचित्र कथा बनी।
00000000000000000
''हाय प्रियो, लुक हियर'' : वनमाला बनाम अनुषा
वह जाड़े की शुरुआत की एक गुनगुनी सुबह का दिन था। वहां सुबह का समय प्रायः शांत और कोलाहल रहित होता था। स्टॉफ रूम में प्रियहरि अकेला बैठा था जब वनमाला ने जाड़े की गुनगुनी धूप की तरह ही हरे पल्लू की पीली साड़ी में एक साथ ही स्टॉफ रूम और प्रियहरि के दिल में इस जगह पहले-पहल प्रवेश किया। वनमाला को देखते ही प्रियहरि को तब ऐसा लगा था जैसे हवा के एक खुश बूदार झोंके में समाई कलकत्ते की वह बंगाली बाला अनुषा दबे पांव उसका पीछा करती उसे चौंकाने सामने आ खड़ी हुई हो। पल भर में ही अनुपस्थित-उपस्थिति की अपनी वैसी प्रभा में समेट प्रियहरि को वह उस जगह उड़ा ले चली थी जो इस वक्त उसकी स्मृतियों को आंदोलित कर रहा था।
सुबह-सुबह हावड़ा के विशाल रेलवे स्टेशन पर वह उतरा था। स्टेशन कैम्पस के बाहर सटे हुए गुमटीनुमा स्टाल पर उसने उतनी सुबह ही गरमागरम इडलियों के साथ चाय ली थी। लंबी यात्रा की थकावट से उस तरह उसने राहत की सांस ली थी। नजर जहां-जहां दौडती गई उसने पाया था कि एक करोड की जनसंखया का कास्मापोलिटन महानगर समझे जाने के बावजूद यहां भी अपनी भीड के साथ वही देहाती भदेसपन बरकरार था जो हिन्दुस्तान के हर बडे-छोटे शहर में अट्टालिकाओं और झोपडियों, भद्रलोक और अकिन्चनवत् जन के बीच पसरा होता था। मुम्बई का महानगर ही एक अपवाद था। वहां की चकाचौंध और उसमें आत्मकेन्द्रित जन के रेले के विपरीत यहां फुटपाथों, बाजारों, गलियों में कस्बाईपन का ठीक वैसा ही माहौल पाया जाता था जैसा उसके अनुभव में बसा था।
आधे किलोमीटर पर ही आवारा सांडों, हाथगाड़ियों, मानव-रिक्शों के साथ तादात्म्य स्थापित किये सडती सब्जियों का ढेर पसरा था और उन सब के साथ सब को चीरकर निकल जाने की कस्मकस में ट्रामों, टैक्सियों, और कारों की चीख दौड रही थी। हाटों, पुकुरों, टोलों, पाडों और सरणियों में पसरे इस महानगर ने जल्द ही उसे भी लील लिया था। बहुत धीरे-धीरे उसकी समझ में आया कि रोशोगुल्ला, रोबिन्द्रो भारती, ऐतिहासिक महत्व के पुस्तकालयों, कालीघाट की स्थायी चहल-पहल, एस्प्लेनेड, प्रेसीडेन्सी कालेज, नन्दन थिएटर और ज्योतिबाबू में रचा-बसी उसकी एक खास संस्कृति है, जो समानता में भी विशिष्टता लिए कोलकाता को अलग पहचान देती है। तब वह भी उसका गुणगान यूं करने लगा था जैसे उस जमीन पर उसका पैदाइशी हक हो। अब वह नवागन्तुकों को वैसी ही चिढ़ाने वाली निगाहों से तौलता जैसा उसे शुरुवाती दिनों में तौला जाता था। वह जैसे बदस्तूर एक नियम था, जिससे हर नवागंतुक को गुजरना होता था। अब उसकी जुबान ने भी वाक्यों और शब्दों के अकारान्त पर ओकारान्त की परत सगर्व चढा ली थी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि अंदर से एकांतिक होता भी समाज और माहौल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए बिना वह चैन से नहीं बैठ सकता था। मार्क्सवादी राजनीति और ट्रेड यूनियन के तौर-तरीकों में रंग चलने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा था।
तकरीबन दो सौ सरकारी-गैरसरकारी कालेजों का नियमन करने वाली यूनिवर्सिटी के अपने दूरस्थ कालेज का वह हिस्सा बन चुका था। अजनबीयत का पहला महीना गुजरते-गुजरते पचास-साठ के स्टाफ वाले उस कालेज का हिस्सा प्रियहरि बन चुका था। जल्द ही अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व से लोकप्रियता और इज्जत हासिल करने में वह सफल हुआ था।
उसका खुद का ठिकाना बहू बाजार की नयी-पुरानी इमारतों के बीच दो कमरों का एक फ्लैट था जो एक सदी से रचे-बसे मारवाडियों की मिल्कियत का एक हिस्सा था। एक-दो को छोड उसकी संस्था का सारा स्टाफ इस मेट्रोपोलिटन के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पच्छिम से लंबी दूरियां पार कर पहंचता था। बहुतेरों के अपने घर थे और कुछ बेघर थे।
शिक्षकों में उनकी अपनी सीमा चाहे जो हो लेकिन कहने के लिये सब की अपनी ठसक थी। काजोल के पास अंग्रेजी के साथ सुहरावर्दी एवेन्यू के लेडी ब्रेबोर्न कालेज से बी.ए में फ्रेंच की डिग्री थी। गार्डन रीच की ओर रहने वाली विभावरी साल्टलेक इलाके के स्काटिश चर्च की स्टुडैन्ट रही आई थी। अनुषा ने मिडिल टाउन के लोरेटो से मैनेजमेन्ट का कोर्स किया था और बैंकिंग की विशेषज्ञा समझी जाती थी। नीहार को गर्व था कि वह प्रेसीडेन्सी कालेज का स्टुडेन्ट था। प्रियहरि जैसे कुछ एक ही थे जो उज्जैन, दिल्ली, बनारस, पटना, रांची से भटकते यहां आ पहुचे थे।
शुरू-शुरू में लगता था कि इस महानगर का यह कालेज भी महान होगा लेकिन जल्द ही प्रियहरि को अनुभव हो गया कि वहां भी माहौल वैसा ही था जैसा देश के किसी भी आम शिक्षा-संस्थान में हुआ करता था। वैसे ही छात्र और छात्राएं, वैसी ही पाठ्यक्रम केन्द्रित तैयारी और पढ़ाई की खानापूरी, वैसे ही छात्रसंघ के चुनावों की हुल्ल्ड , वैसी ही हडतालें और वैसे ही समझौते जैसे हर जगह हुआ करते थे। यहां की राजनीति और जगहों से कुछ अधिक गरम हुआ करती थी। बात-बात पर इलाके के नेताओं से लेकर बडे समझे जाने वाले नेता तक दिलचस्पी लेते यूं दखल देते जैसे कोई राष्ट्रीय मसला आ खडा हुआ हो। कुछ ही सालों में प्रियहरि का मन उचाट हो चला था।
उस एक दिन वह बी.बी.डी बाग से पैदल ही चौरंगी तक चला आया था कि किसी एक परिचित स्वर का सांगीतिक लय कानों से उलझ गई -
'' हाय प्रियो, लुक हियर ''
प्रियहरि ने पलटकर नजर दौडाई। करीब ही उसे सुनहले किनारों से सजी हरी साडी और कुसुम्भी छींटदार ब्लाउज में कसा वह चेहरा दिखाई पडा जिस पर कंधे तक लहरातीं केशराशि और माथे पर जुल्फ की लटें लहरा रही थीं।
'' तुम देखते ही नहीं। कब से तुम्हें देखती मैं हाथ हिलाये जा रही हूँ।''
'' मुझे क्या मालूम ओन्नी डियर कि तुम यहां शापिंग कर रही हो।''
यह अनुषा थी। स्टाफ में सब से निराली और बेहद नफासत-पसंद समझी जाती थी। गप्पों से उसे नफरत थी। ऐसा कभी-कभार होता जब अनुषा और प्रियहरि के साथ-साथ मिल बैठने का संयोग होता। चर्चा में राजनीति और कल्चर ही ओन्नी की रुचि के विषय थे। जब कभी मौका और फुरसत के लम्हे मिलते, दोनों के बीच खूब बातें होतीं। लगाव तो जाहिर था लेकिन प्यार-व्यार के चक्कर तक पहुंचने से रह गया था।
वे साथ-साथ एस्प्लेनेड की तरफ बढ़ चले थे। अनुषा के हाथ का थैला प्रियहरि ने थाम लिया था। चलते-चलते अनुषा ने शिकायत की-